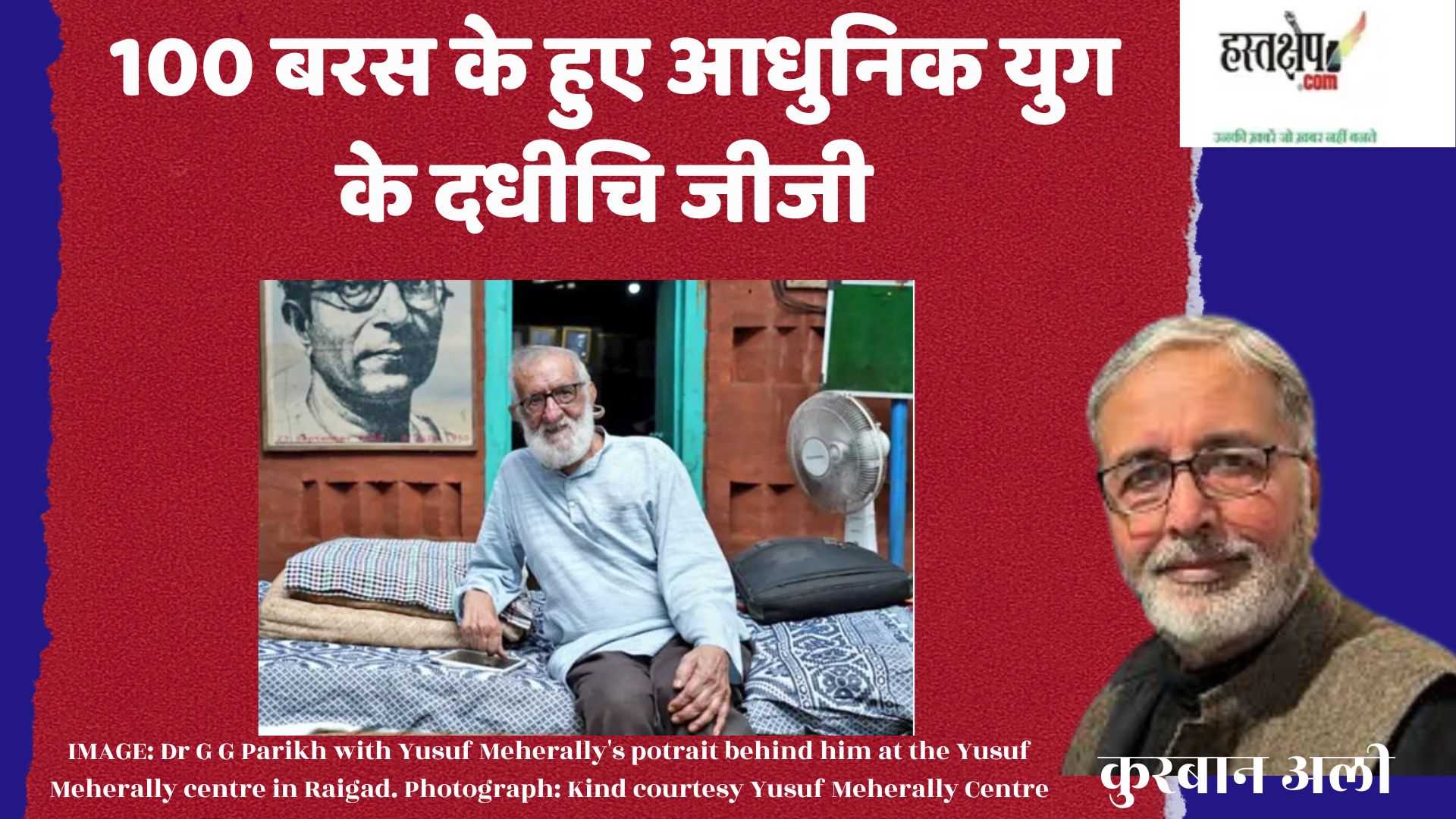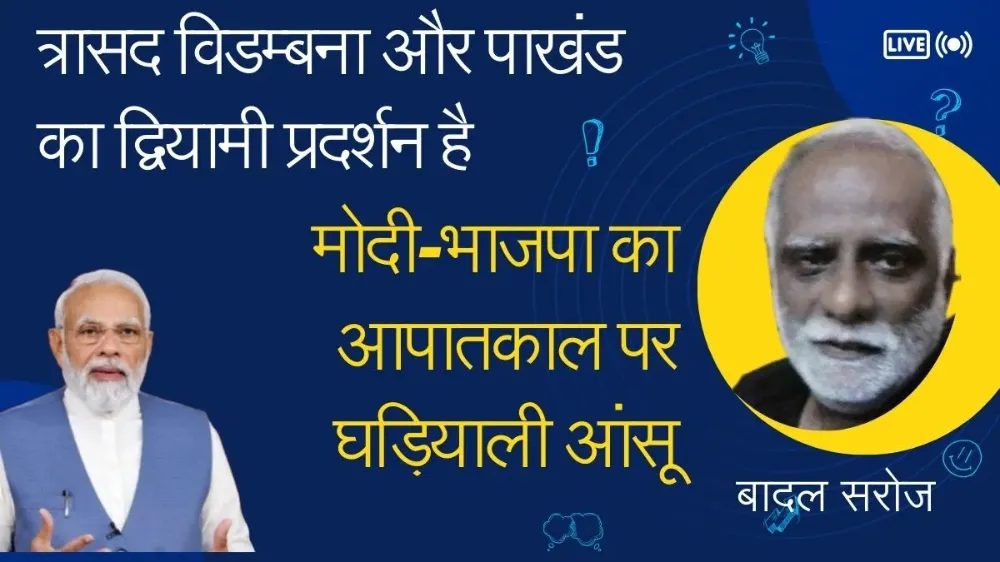Book Review of The Disruptor: How Vishwanath Pratap Singh Shook India Book by Debashish Mukerji in Hindi | देबाशीष मुखर्जी की पुस्तक द डिसरप्टर: हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया की समीक्षा हिंदी में
विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्हें अधिकांश लोग वीपी सिंह के नाम से जानते हैं, वह 7 अगस्त 1990 के बाद से भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक रहे हैं जिन्हें यहां के ‘संभ्रांत’ समाज ने सबसे अधिक गालियां दीं और उनके निधन के लगभग 12 वर्षों के बाद इस समाज ने उन्हें माफ नहीं किया। हालांकि इससे पहले उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था और काशी के ब्राह्मणों ने वास्तव में उन्हें 'राजर्षि' की उपाधि से सम्मानित किया था।
और 7 अगस्त 1990 को नायक से खलनायक बना दिए गए वीपी सिंह..
7 अगस्त 1990 को संसद में मंडल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति उसके बाद से राजनीतिक टिप्पणीकारों ने उन्हें नायक से खलनायक बना दिया और फिर उन्हें भुलाने के पूरे प्रयास किए और उनके केवल उस हिस्से को याद रखा जो उनके लिहाज से ‘जातिवादी’ था।
यह कोई आश्चर्य नहीं है मंडल आंदोलन के दौरान उत्तर भारत की सड़कों पर पैदा हुई 'अराजकता' के अलावा कुछ भी याद नहीं था लेकिन उस अराजकता को हमारे मीडिया ने देश पर ‘अत्याचार’ और ‘अन्याय’ बताया। विश्वनाथ प्रताप भारत के सबसे बड़े ‘जातिवादी’ हो गए जिन्होंने एक ‘सेक्युलर देश में ‘जाति’ का सवाल खड़ा करके ‘भोली भाली’ सवर्ण आबादी का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया।
लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि सवर्ण या सवर्ण नेता, बुद्धिजीवी और राय बनाने वालों ने तो वीपी को 'मंडल पाप' के लिए जिम्मेदार माना ही, इससे लाभान्वित होने वाले ओबीसी नेताओं ने न तो
आश्चर्य तो यह है कि मण्डल के 30 वर्षों बाद भी बाकी सभी नेता इसका क्रेडिट ले रहे हैं लेकिन वीपी सिंह को ये क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं हैं जिसके फलस्वरूप उनकी राजनीति संभवतः खत्म ही हो गई।
एक कार्यक्रम में वीपी ने कहा था कि ‘मैंने अपना पैर भले ही तुड़वा लिया लेकिन मैं गोल करने में कामयाब हो गया।। अब सभी राजनीतिक दलों को मंडल-मंडल का जाप करना होगा'।
वीपी सिंह की सादगी और ईमानदारी उनका एक हथियार भी थी और कमजोरी भी
वीपी सिंह की सादगी और ईमानदारी (Simplicity and honesty of VP Singh) एक शक्तिशाली हथियार थी, लेकिन यह उनकी कमजोरी भी थी और यही कारण है कि 30 साल बाद कार्यान्वयन का श्रेय उनके चतुर मित्रों ने स्वयं ले लिया लेकिन उन्हें आज तक नहीं दिया। उनमें बहुत तो ऐसे थे जो वास्तव में उस महत्वपूर्ण क्षण में उनसे अलग हो गए थे।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन (Implementation of Mandal Commission Report) के समय शरद यादव और रामविलास पासवान वीपी सिंह के दो सबसे मजबूत सहयोगी थे, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कि उन्होंने इन्हें केवल चेकमेट देवी लाल के लिए लागू किया, जो उनके उपप्रधानमंत्री थे।
कैबिनेट से बर्खास्त होने का मतलब है कि हम आदमी और उसकी ईमानदारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इस पुस्तक में दो ऐसे दृष्टांत हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि वीपी इसके लिए कितने तैयार थे। उनके अभिन्न मित्र सोमप्रकाश ने बातचीत में बताया के मण्डल आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए वीपी ने चौधरी देवी लाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई क्योंकि यह जनता दल के चुनाव घोषणापत्र (Janata Dal Election Manifesto) का हिस्सा था लेकिन महीनों गुजर जाने के बाद भी समिति की कोई एक बैठक भी नहीं हो पाई थी। इसका मुख्य कारण यह था के जाट मण्डल की सिफ़ारिशों में पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किए गए थे इसलिए इस रिपोर्ट के सिलसिले में देवीलाल को कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी।
मार्च 1990 तक जब इस कमिटी ने कोई काम नहीं किया तो वीपी ने राम विलास पासवान से बातचीत कर इस बात को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को कहा।
नेता लोग तो अपनी राजनीतिक स्थितियों के अनुसार बात करते हैं लेकिन मण्डल सिफ़ारिशों के लागू होने के सबसे बड़े गवाह थे श्री पी एस कृष्णन, जो उस समय केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव थे और आरक्षण और दलितों के अधिकारों के प्रश्न पर काम करने वाले लोगों में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे, वह बताते हैं कि उन्हें पता था का इस सरकार का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होने वाला इसलिए उन्होंने 1 मई 1990 को कैबिनेट के लिए एक नोट में ये बात रखी थी कि इसके लिए केवल एक शासनदेश की आवश्यकता है, संसद जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े अधिकारियों ने शायद इससे सहमति नहीं व्यक्त की फिर भी ये नोट वीपी सिंह के पास पहुँच गया और उन्होंने तुरंत ही राज्यों को इस संदर्भ में लिख दिया हालांकि मण्डल लागू करने का आधिकारिक फैसला 2 अगस्त 1990 को लिया गया।
कृष्णन कहते हैं 16 नवंबर 1992 को जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले केस में मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय को संवैधानिक तौर पर सही माना तो वीपी सिंह ने उन्हें फोन करके बताया : “यदि मैं अभी मर भी गया तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट होकर मरूँगा।“।
कृष्णन कहते हैं, “वह वैचारिक तौर पर बहुत निष्ठावान थे जो आज के दौर के नेताओं में तो बहुत कम देखने को मिलती है”।
हममें से जो वीपी सिंह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से उनकी राजनीति का अनुसरण कर रहे हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वह एक अपरंपरागत राजनेता थे और उनमें निश्चित रूप से 'आदर्शवाद' और 'शिष्टता' की भावना थी, लेकिन इसकी भी कई लोगों ने आलोचना की थी। कई दिग्गज उन पर पाखंडी होने का आरोप लगाते थे तो बहुत के लिए वह एक 'अवसरवादी' थे जिन्होंने ओबीसी के 'नेता' बनने के लिए 'मंडल आयोग' का इस्तेमाल किया, जबकि अन्य ने सोचा कि वह अपने विरोधियों के साथ चले गए हैं और वोट की राजनीति के लिए अपने समुदाय के हितों की अनदेखी कर रहे हैं।
वीपी सिंह के बारे में जानना क्यों जरूरी है? | Why is it important to know about VP Singh?
बामसेफ और बसपा के आख्यान में भी, मंडल आयोग की रिपोर्ट को पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम द्वारा बनाए गए दबाव के कारण लागू किया गया था। सवर्णों में से कई के लिए वह एक नकली राजपूत थे और जयचंद की संतान थे जिसने भारत में 'मुगल' शासन लाने के लिए अपने ही जाति के योद्धा को धोखा दिया। इसलिए, वीपी सिंह के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतने वर्षों के सार्वजनिक जीवन में बेदाग होने के बावजूद उन्हें अभी भी एक बहुत गलत समझा गया, जिन्हें न तो अपने जीवनकाल में और न ही उनकी मृत्यु के बाद उनका हक मिला।
सार्वजनिक हस्तियों विशेषकर राजनीतिक नेताओं को उनके एक कार्य नहीं आंका जा सकता क्योंकि कई लोग इसे पसंद करेंगे और कई अन्य इससे असहमत हो सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की विचारधारा को उसके सम्पूर्ण जीवन के कार्य और पृष्ठभूमि से समझना महत्वपूर्ण है।
वीपी सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास ''नहीं था वो जनता नहीं थी जो उन्हें याद कर सके, हालांकि यही जनता उनके लिए ‘राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है कि नारे लगाती थी’।
मंडल के लिए ब्राह्मणवादी बुद्धिजीवियों ने उनका तिरस्कार किया क्योंकि उन्होंने अपने समाज के साथ ‘धोखा’ दिया और ओबीसी दलितों के लिए वो मान्य नहीं थे क्योंकि वह उनकी बिरादरी से नहीं थे इसलिए उल्लेख के लायक नहीं माना गया। उनके पास उनके सिद्धांतों या विचारों को आगे करने या उनको याद करने के लिए कोई पार्टी या संस्था भी नहीं थी।
Biography of Vishwanath Pratap Singh in Hindi | विश्वनाथ प्रताप सिंह की जीवनी हिंदी में
अनुभवी पत्रकार सीमा मुस्तफा की द लोनली प्रोफेट और 'मंज़िल से ज्यादा सफर' जो राम बहादुर राय द्वारा उनके साथ साक्षात्कार पर आधारित थी, लेकिन ये दोनों किताबें वीपी सिंह के सम्पूर्ण सामाजिक राजनीतिक व्यक्तित्व (Complete socio-political personality of VP Singh) के साथ न्याय नहीं करतीं।
देबाशीष मुखर्जी की किताब ‘द डिसरपटर’ वीपी सिंह पर लिखी गई अभी तक की सबसे सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। इससे यह महसूस होता है कि वीपी सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल (VP Singh's tenure as Prime Minister) हालांकि बहुत छोटा था लेकिन 1980 से लेकर 2008 तक वह भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं में से एक थे और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता था।
वीपी सिंह को समझने के लिए उनके बचपन और युवा अवस्था के दिनों को समझना होगा। दरअसल वह अपने दत्तक पिता मांडा के राजा राम गोपाल सिंह और अपने जैविक पिता दैया के राजा भगवती सिंह के बीच की तनातनी में फंसा रहा। बचपन से ही एक असुरक्षा की भावना उनके दिमाग में आ गई थी। उनके दत्तक पिता ने उन्हें उनके जैविक माता पिता से मिलने से भी इनकार कर दिया था। वह हमेशा सुरक्षा के घेरे में रखते थे और उनका खान भी सुरक्षा कारणों से पहले चखा जाता था, क्योंकि राज परिवार के इकलौते वारिस थे। उन्होंने अक्सर अपनी सामंती परवरिश को यह कहते हुए दर्शाया है कि 'अगर उनके क्षेत्र और संपति पर रहने वाले किसी व्यक्ति को कोई समस्या थी और उसने मदद मांगी, तो मेरे पिता ने यह महसूस किया, इसे प्रदान करना उनका कर्तव्य था'।
उनका जीवन अत्यंत कठिन था क्योंकि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि उनके प्राकृतिक माता-पिता को भी नहीं। यद्यपि उनका परिवार गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ था, लेकिन वीपी सिंह उनसे प्रभावित थे और उन्होंने विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।
उनके जीवन की असुरक्षा ने शायद उन्हें एक दार्शनिक राजनीतिज्ञ बना दिया क्योंकि 'एक राजा के परिवार में पैदा होने के कारण उन्हें केवल अकेलापन और शर्मिंदगी मिली थी'। वह अपने परिवार की समाप्ति के विषय में असहज थे। वह अपने बड़े भाई संत बख्श सिंह से प्रभावित थे, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे और जिनके पास एक विशाल पुस्तकालय था।
वीपी सिंह ने छात्र राजनीति में आते-आते, इस तथ्य के बावजूद कि उनका परिवार इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सामंत था, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था जो उनके पिता राजा भगवती सिंह के लिए बहुत ही निराशा और पीड़ादायी था।
विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित वीपी सिंह ने न केवल 'सर्वोदय' आंदोलन की विभिन्न गतिविधियों और 'श्रमदान' जैसे रचनात्मक कार्यों में भाग लिया बल्कि पासना गांव में लगभग 150-200 एकड़ 'पूर्णतः सिंचित भूमि' भी भूदान के तहत दान कर दी। उनके परिवार के सभी सदस्य उनसे नाराज थे और विनोबा भावे ने भी उन्हें समझाने के प्रयास किए कि वह तो मात्र अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा ही मांग रहे थे लेकिन 'वीपी पहले से ही इसके लिए तैयार थे। उनके जैविक पिता भगवती सिंह को इस बात से गहरा धक्का लगा और इससे वह सावधान हो गए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दैया में 900 एकड़ जमीन भी उसी तरह से भूदान में चली जाए। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में इसे लटकाए रखा। क्योंकि वीपी दइया राज घराने के अकेले कानूनी वारिस थे इसलिए अंततः वह जमीन उनके ही नाम आई लेकिन उन्होंने इस जमीन को नहीं लिया और जमीन दैया ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि मांडा में राज परिवार द्वारा गोद लेने के बाद अपने प्राकृतिक परिवार से कुछ भी नहीं चाहते हैं।
जवाहर लाल नेहरू से प्रभावित रहे वीपी सिंह
छात्र राजनीति से लेकर राजनीति में वीपी सिंह के शुरुआती दिनों में जवाहर लाल नेहरू से प्रभावित रहे जिनके लिए उन्होंने फूलपुर में चुनाव प्रचार किया, और नेहरू जी की मृत्यु की बाद वह इलाहाबाद में लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े और बड़े भाई संत बख्श सिंह के प्रचार से उन्होंने चुनावी राजनीति की बारीकियों को समझा। सर्वोदय के साथ उनके सामुदायिक कार्य ने उन्हें अपने क्षेत्र में दलितों के साथ जुड़े। वह जवाहर लाल नेहरू से अत्यधिक प्रभावित थे और स्थानीय नेताओं की 'शत्रुता' के बावजूद उनके लिए प्रचार किया। बाद में, वह लाल बहादुर शास्त्री के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े और ललिता शास्त्री को माण्डा में अपने राजमहल के किले से 'लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन' शुरू करने की अनुमति दी।
उन्होंने 1967 में एक उपचुनाव में सरांव निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। एक विधायक के रूप में, उनकी पहली सफलता राज्य के शक्तिशाली मुख्यमंत्री चंद्र भानु गुप्ता द्वारा उनके क्षेत्र के प्रदर्शनकारी किसानों की मांग को स्वीकार करना था, जिन्होंने पार्टी से उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया था।
वीपी सिंह ने खुद को आम लोगों के मुद्दों से परिचित रखा जिसका लेखक ने इस पुस्तक में खूबसूरती से वर्णन किया है, "वीपी अक्सर गांव गांव की यात्रा करते थे, और ग्रामीणो की समस्याओं को नोट करते रहते थे। ऊनके पास एक एक सेकेंड हैंड जीप थी जिसे वह स्वयं चलाते थे क्योंकि वह कहते थे के केवल वह ही उसे संचालित कर सकते थे। उस प्री-लैपटॉप/स्मार्टफोन युग में, वह विभिन्न गांवों की समस्याओं की सही जानकारी रखने के लिए वह इंडेक्स कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे जिसे वह समय-समय पर अपडेट करते रहते थे। प्रत्येक कार्ड एक विशेष विभाग को समर्पित था, जिस पर गाँवों के नाम और उस विभाग से संबंधित उनकी विशिष्ट समस्याएं दर्ज की जाती थीं।
वह बताते हैं, 'इस तरह इलाहाबाद जिला प्रशासन या लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान मेरी उंगलियों पर हमेशा डेटा होता था'।
इसी अवधि के दौरान, उनके निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांवों में दलितों ने अपने 'पारंपरिक काम' को नहीं करने का फैसला किया, जैसे कि शवों का निपटान और अन्य जाति की महिलाओं को उनके प्रसव में मदद करने के लिए दाई के रूप में काम। दलितों के इनकार को उच्च जाति ने हल्के में नहीं लिया और उन्होंने उनके आर्थिक बहिष्कार की धमकी दी थी। वीपी ने दोनों पक्षों से बातचीत की और इस समस्या का समाधान निकाला। और कहा कि 'आप किसी को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वह नहीं करना चाहता'।
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोक सभा का अपना पहला चुनाव फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से अनुभवी समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा को हराकर जीता जिनका रवैया शुरू से ही उनके प्रति बहुत तिरस्कारपूर्ण था। 10 अक्टूबर, 1974 को प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें केन्द्रीय वाणिज्य उप मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जहां मंत्रालय में उनके बॉस पश्चिम बंगाल के एक महान दार्शनिक राजनीतिज्ञ देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय थे।
वीपी को विदेश एवं वाणिज्य के सवालों में बहुत दिलचस्पी थी। इसी पुस्तक से पता चला कि कनिष्ठ मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की और उत्तरी कोरिया की राजधानी में लगभग एक सप्ताह तक रहे।
आपातकाल के दौरान वह इंदिरा गांधी के साथ ही जुड़े रहे लेकिन तब वे बहुत कनिष्ठ मंत्री थे और शायद उनके एहसान तले भी दबे रहे इसलिए उस समय उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी।
1977 के आम चुनावों में वीपी को जनेश्वर मिश्रा ने भारी मतों से हरा दिया। लेकिन ये तो पूरे उत्तर भारत में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के विरोध की भारी आंधी थी, जिसमें वह स्वयं भी रायबरेली से चुनाव हार गई थीं।
1980 देश में मध्यावधि चुनावों के चलते सत्तारूढ़ जनता पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई और लोगों ने इंदिरा गांधी और काँग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताया। वीपी ने पुनः फूलपुर से भारी मतों से जनेश्वर मिश्र को पराजित किया।
इसी वर्ष जून में हुए चुनावों में जब काँग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती तो काँग्रेस नेतृत्व में वीपी सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर लखनऊ भेजा। इस प्रकार वीपी सिंह इलाहाबाद की स्थानीय राजनीति से प्रदेश और देश की राजनीति में जाने जाने लगे।
दरअसल वीपी सिंह के राजनीतिक जीवन को वास्तव में चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1980 उनके उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनने के पहले, फिर केन्द्रीय मंत्री से लेकर जन मोर्चा तक का सफर, फिर जब वे नवंबर 1989 में प्रधान मंत्री बने और फिर नवंबर 1990 में पद छोड़ने के बाद जब उन्होंने फिर से जनोन्मुखी राजनीति करना शुरू किया।
अधिकांश बुद्धिजीवी और राजनीतिक टिप्पणीकार 1980 से पहले के उनके जीवन और कार्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, जिसे इस पुस्तक के लेखक ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। मुख्यमंत्री के पद पर उनका उत्थान आश्चर्यजनक था लेकिन उनके कार्यों ने विशेषकर उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने बांदा जिले के तिंदवारी से राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने पर मोटरसाइकिल और सार्वजनिक परिवहन में प्रचार करने का फैसला किया। उनके प्रतीकवाद ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि चुनाव में उनके सभी प्रतिद्वंद्वियों की जमानतें जप्त हो गईं।
उप्र के मुख्यमंत्री के रूप में वीपी सिंह की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वीपी की सबसे बड़ी चुनौती डकैतों का बढ़ता खतरा था, जिसके परिणामस्वरूप उनके बड़े भाई चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की भी हत्या हुई, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 14 फरवरी 1981 को बेहमई में फूलन देवी और उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर ठाकुर समुदाय के 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 3 मई 1981 को महावीर पोथी और उसके गिरोह के सदस्य ने भूमि विवाद को लेकर आगरा के कुंवरपारा गांव में 22 दलितों की हत्या कर दी। छवि राम गिरोह ने 8 अगस्त 1981 को 9 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। संतोषा सिंह और राधे मैनपुरी जिले के देहुली गांव में श्याम ने 24 दलितों की हत्या कर दी। इसके अलावा साधुपुर में 10 दलितों का नरसंहार हुआ था लेकिन सबसे बड़ा संकट मुरादाबाद सांप्रदायिक दंगा था जिसमें लगभग 250 लोग मारे गए थे। श्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में 5000 से अधिक लोगों को मारने का आरोप लगाया, जिनमें ये कहा गया कि ज्यादातर ओबीसी थे।
उत्तर प्रदेश में प्रशासन में कुशासन के चलते वीपी सिंह के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहना मुश्किल हो रहा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
दरअसल, काँग्रेस की संस्कृति के अलग हट कर, वीपी ने जब पहले त्यागपत्र दिया तो काँग्रेस हाई कमांड ने उसे नामंजूर कर दिया। काँग्रेस संस्कृति में कोई अपनी मर्जी से भी त्यागपत्र नहीं देता था और जिसे जबरन त्यागपत्र लिखवाया जाता था वो भी यही कहता है कि जनता की भावनाओं का ध्यान रखकर ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन वीपी ने जब देखा कि परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं क्योंकि पार्टी में अलग धडे थे जिन्हें कही न कही केंद्र में बैठे नेता शह देते हैं तो उन्होंने दूसरा इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेज दिया। त्याग के इस कार्य ने वास्तव में एक ईमानदार राजनेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत करने में मदद की।
काँग्रेस में उस समय तक गांधी परिवार के अतिरिक्त किसी को भी ऐसा करने का ‘अधिकार’ नहीं था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी ईमानदारी का सम्मान करते हुए उन्हें केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्री बनाया। वीपी ने अपने ऊपर दी गई जिम्मेवारी को गंभीरता से लिया और कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गैट से संबंधित सम्मेलनों और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ( अंकटाड) में भाग लिया।
दिसंबर 1984 के अंत में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बुलाए गए आम चुनाव में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में भारी जनादेश जीता क्योंकि विपक्ष का पतन हो गया। वीपी सिंह को केंद्रीय वित्त मंत्री बनाया गया।
वीपी सिंह की आर्थिक नीतियों की समीक्षा (Review of VP Singh's economic policies)
1985 और 1986 में वीपी सिंह का बजट अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और 'लाइसेंस परमिट राज' को खत्म करने की दिशा में भारत का पहला प्रयास था। इस पुस्तक में वीपी की आर्थिक नीतियों और वित्त मंत्री के तौर पर उनके निर्णयों को बारीकी से जांचा परखा है। उन्होंने आयकर की दरो को 62% से घटाकर 50% कर दिया और आयकर छूट की सीमा बढ़ा दी। उन्होंने MODVAT संशोधित मूल्य वर्धित कर भी पेश किया जिसे मीडिया ने बहुत सराहा। मीडिया द्वारा वीपी सिंह की प्रशंसा की गई, लेकिन जल्द ही सिस्टम को 'साफ' करने के उनके प्रयासों ने उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया क्योंकि औद्योगिक घरानों की टैक्स चोरी के उनके अभियान को मीडिया ने 'रेड राज' करार दे दिया और मीडिया ने इसकी जम कर आलोचना की थी। काँग्रेस के कुछ नेताओ और उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री से उनकी शिकायत कर दी थी क्योंकि ललित मोहन थापर, किर्लोस्कर, विजय माल्या सहित कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों की गिरफ्तारी हुई थी।
वीपी सिंह पर संयुक्त राज्य अमेरिका की निजी जासूसी एजेंसी फेयरफैक्स को बड़े औद्योगिक घरानों की कर चोरी की जांच के लिए आमंत्रित करके भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया गया था।
इस अवधि के दौरान राजीव गांधी के साथ उनके संबंध खराब हो गए लेकिन राजीव को अंदाज हो गया था कि वीपी सिंह की छवि जनता में बहुत अच्छी हो चुकी है और इसलिए वो उन्हें सीधे-सीधे नहीं हटाना चाहते थे अपितु उनको ‘नियंत्रित’ करना चाहते थे। बहुत चालाकी से उन्हें इस बहाने वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और वहां एक सक्षम मंत्री की जरूरत है। वीपी सिंह ने वहां भी एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी सौदे में भ्रष्टाचार पाया और जांच का आदेश दिया। इसने राजीव गांधी और वीपी सिंह के साथ और मतभेद पैदा कर दिए, अंततः 11 अप्रैल, 1987 को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
कुछ दिनों बाद बोफोर्स स्कैन्डल लाइम लाइट में आ गया जिसमें राजीव गांधी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ये मुद्दा 1989 के चुनावों का मुख्य मुद्दा बना।
इस्तीफ़ों ने हमेशा ही वीपी सिंह के चारों ओर एक बड़ा प्रभामंडल बनाया क्योंकि लोग ये मानने लगे थे कि यह आदमी सत्ता का लोभी नहीं है और उनके इस्तीफे ने राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि को और धूमिल कर दिया। उस समय तक कांग्रेस की संस्कृति चाटुकारिता थी और यहां पार्टी ने बड़ी गलती की क्योंकि छोटे नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से वीपी सिंह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया। राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उनकी सभाओं में बाधायें पैदा करने की कोशिश की लेकिन इस अवधि ने दर्शाया कि वीपी सिंह न केवल महान सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, बल्कि एक अत्यंत समझदार और परिपक्व व्यक्ति भी थे। काँग्रेस ने उन पर जितने हमले किए, वीपी का व्यक्तित्व और निखर गया और राजीव गांधी उनके सामने अपरिपक्व नजर आए।
जिन लोगों को राजीव गांधी से हिसाब पूरा करना था वे भी उनकी सरकार को अव्यवस्थित करना चाहते थे। यह समझना जरूरी है कि इससे बाहर संकट पैदा करने के प्रयास किए गए थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर 'अनदेखा' महसूस कर रहे थे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रहे थे। वह कानूनी जानकारों से परामर्श कर रहे थे कि क्या भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति के साथ संवाद करने की संवैधानिक प्रथा का पालन नहीं करता है।
देश के दो नामी गिरामी संपादकों के बीच राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर ये बहस चल पड़ी थी। इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शौरी राष्ट्रपति को सलाह दे रहे थे कि वह प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं तो दूसरी और टाइम्स ऑफ इंडिया में गिरी लाल जैन इसके विरोध में थे। ये अलग बात है कि मण्डल के बाद दोनों ही हिन्दुत्व के कैम्प के प्रमुख ‘चिंतक’ बन गए।
राष्ट्रपति जैल सिंह न केवल इन बातों पर कानूनविदों से चर्चा कर रहे थे बल्कि कांग्रेस के असंतुष्टों जैसे वी सी शुक्ल और अरुण नेहरू के साथ लगातार संपर्क में थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। वीपी सिंह की लोकप्रियता और राजीव गांधी के साथ उनके मतभेदों के चलते ज्ञानी जी ने उन्हें यह संदेश भिजवाया कि यदि वह वैकल्पिक सरकार का नेतृत्व करने को तैयार हैं तो वह उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं लेकिन वीपी सिंह ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया।
इस पुस्तक में इस बात पर विस्तृत चर्चा है लेकिन अरुण शौरी, इंडियन एक्स्प्रेस की पत्रकारिता, एम जे अकबर की अवसरवादी पत्रकारिता पर भी चर्चा करना जरूरी था, जो बहुत कम हुई है।
वीपी सिंह पर अक्सर उनकी आलोचना द्वारा 'महत्वाकांक्षी' और 'अवसरवादी' होने का आरोप लगाया गया है, लेकिन समीक्षा के तहत पुस्तक का सावधानीपूर्वक अध्ययन आपको उस व्यक्ति का जीवन न केवल आकर्षक लगता है अपितु प्रेरणादायी भी है जो सत्ता के लिए राजनीति में नहीं हैं। अक्सर उनकी वैचारिकी को लेकर प्रश्न होते थे जैसे वह केवल एक राजनेता थे लेकिन हकीकत यह है कि 31 जुलाई 1955 को वीपी सिंह छात्रों और युवाओ के अन्तराष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने पोलैंड की राजधानी वारसा गए। ये कार्यक्रम लोकतान्त्रिक युवाओं के अन्तराष्ट्रीय फेडरेशन ने किया था जो कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक संगठन था। सर्वोदयी लोगों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और बाद में अम्बेडकरवादियों से भी उनके संबंध बेहतर हुए। दलित पैंथर के संस्थापकों राजा ढाले और जे वी पँवार ने मेरे साथ बातचीत में उन्हें बहुत सम्मानपूर्वक याद किया।
यह पुस्तक एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में झाँकने का प्रयास है जो न केवल एक परिपक्व राजनेता थे बल्कि एक अत्यंत संवेदनशील आत्मा, एक कवि और एक कलाकार भी था।
यूपीए के गठन के दौरान भी ऐसी स्थिति आई जब समूचा विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन वीपी सिंह ने इसको भांप लिया और वह अपने घर से ही गायब हो गए। उस दिन वह रिंग रोड के चक्कर काटते रहे और एक पारिवारिक मित्र के यहां चले गए और सिक्योरिटी को बता दिया कि लोगों को इसकी जानकारी न देना। नतीजा यह हुआ कि विपक्षी नेताओं को इस पद के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवगौड़ा को चुनने के लिए मजबूर किया।
लोग विभिन्न मुद्दों पर राजनीति में बहस पैदा करने और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने में वीपी सिंह के भारी योगदान की उपेक्षा करते हैं। उन्हें केवल मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले उनके बहुत से अन्य महत्वपूर्ण योगदान को भूल जाते हैं। उनके लिए मंडल आयोग जनता दल पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप पूरा करने की प्रतिबद्धता थी। ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जो इस पुस्तक में भी उस तरीके से नहीं आए हैं जैसे आने चाहिए थे। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न देना, अनुसूचित जाति से बौद्ध धर्मांतरितों को आरक्षण देना जो अम्बेडकरवादियों के लिए एक अत्यंत भावनात्मक मुद्दा था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफे के बाद, वीपी ने सरकार द्वारा मंडल रिपोर्ट को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए देश भर में यात्रा की क्योंकि सरकारें उसे लागू करने के लिए राजी नहीं थी। सिवाय तमिलनाडु की डी एम के सरकार के, अन्य राज्यों और नेताओं ने तो मण्डल का नाम लेंगे में समय लगाया।
आखिर में 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके मण्डल फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया।
बाद में वीपी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए संघर्ष किया और मानरेगा और सूचना अधिकार आंदोलन से भी जुड़े। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉ केआर नारायणन को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति वीपी ही थे और एक बार उन्होंने कह दिया तो सभी पार्टियों को उस बात को मानना पड़ा।
हालांकि वी.पी. सिंह के जीवन चक्र को कैद करना कठिन था, लेकिन इस पुस्तक के लेखक ने उन क्षणों को विस्तृत तौर पर दस्तावेजित और कालानुक्रमिक रूप से चित्रित किया है जो अभी तक लोगों की नजर से बाहर थे।
वीपी सूचना के अधिकार के अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सक्रिय भागीदार थे। एक कार्यकर्ता के रूप में, मैंने कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया कि वह अतिथि थे और पूरे दिन चर्चाओं में बैठ रहे।
झुग्गीवासियों के अधिकारों के लिए उनका काम अनुकरणीय है। मैं उनके अपने छात्र जीवन से देख सुन रहा था। वह अनिवार्य रूप से एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे जो बिना किसी 'सुरक्षा' ताम जहां और बिना किसी अहंकार के लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे। अक्सर ऐसे उच्च पदों पर आसीन नेताओं के साथ साथ उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं लेकिन वीपी ने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया था।
वीपी सिंह की जीवन कहानी के साथ-साथ उनके राजनीतिक हस्तक्षेपों को न केवल और अधिक समझने की आवश्यकता है अपितु उनकी राजनीति के ऊपर शोध भी होने चाहिए। उस समय, जब सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तेजी से गायब हो रही है और राजनीतिक नेता समझौतापरस्त हो गए हैं ऐसे में वीपी सिंह की राजनीति एक नखलिस्तान कि तरह थी जिनकी मुख्य ताकत उनकी ईमानदारी और सरलता थी। उनकी वैचारिक राजनीति उन्हें कहीं नहीं ले गई क्योंकि न तो ओबीसी ने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया और न ही राजपूतों ने उन्हें अपना माना जिन्होंने अपने 'मंडल' पाप से विश्वासघात महसूस किया। अन्ना हज़ारे के ‘भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया जबकि देश के इतिहास में वह अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने ऊंचे पदों पर हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और उसके लिए कुर्सी को भी ठोकर मार दी तब भी सवर्णों को ये पसंद नहीं था क्योंकि अन्ना की टीम के अधिकांश सदस्य आरक्षण विरोधी थी। वीपी शायद एकमात्र राजनीतिक नेता हैं जिनके परिवार को राजनीति में आने का विशेषाधिकार नहीं मिला। उनके नाम पर एक भी सड़क, स्कूल या स्मारक नहीं है। मण्डल से उपजे लोग भी उन्हें याद नहीं करते। हाँ बी पी मण्डल को खूब याद करते हैं, बिना ये जाने कि यदि वीपी नहीं होते तो मण्डल की रिपोर्ट कहां होती और कौन बी पी मण्डल को याद करता।
दरअसल यदि वीपी सिंह जैसे लोगों की वैचारिक राजनीति विफल हो जाती है तो किसी भी सरकार में दूसरे समाजों के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको केवल अपनी बिरादरी का ही सवाल उठाना है। आज राजनीति उसी में बदल चुकी है और नतीजा है अस्मिताओं के नाम पर जातियों के कुछ स्वयंभू नेताओ की भरमार जो एक बार राजनीति में स्थापित होने के बाद अपने परिवारों को ही स्थापित कर रहे हैं।
जब वीपी की राजनीति असफल होती है तो आदित्यनाथ जैसे लोग चलेंगे क्योंकि वे अपने-अपने समाजों के हित करें या न करें लेकिन ऐसी इमेज तो क्रीऐट कर देते हैं। अब राजनीति अपनी अपनी जातियों के ‘हितों’ तक सीमित रह गई है जिसमें हाशिए या कम संख्या वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।
मंडलोपरांत राजनीति में क्या कभी कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाए हैं ?
हालांकि यह पुस्तक वीपी सिंह के व्यक्तिगत मित्रों और उनके नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे गए विस्तृत इंटरव्यू पर आधारित है फिर भी कुछ बाते ऐसी हैं जिन्हें विस्तृत तौर पर लिखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के कार्यकाल में अव्यवस्था का क्या कारण रहा होगा। और उनके डकैती विरोधी अभियान को मूलायम सिंह ने क्यों ‘पिछड़ी जातियों’ के विरुद्ध अभियान कहा। मीडिया की भूमिका और अरुण शौरी एवं एम जे अकबर के रोल को भी खंगालना चाहिए था। अकबर ने वीपी सिंह के खिलाफ फर्जी रिपोर्टें फाइल की थीं, जैसे सेंट किट्स में उनका खाता था और वो मात्र टेलीग्राफ तक सीमित नहीं रही थीं अपितु दिल्ली के कुछ अखबारों में भी अकबर को लिखने की आजादी मिली हुई थी।
तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये छूटा कि वीपी सिंह राजनीति में नैतिकता के पक्षधर थे और ये उनके दुश्मन भी मानते होंगे कि बेहद ईमानदार थे और भ्रष्टाचार को राजनीति के केन्द्रबिन्दु में लाने वाले पहले राजनेता थे लेकिन अन्ना हज़ारे हों या केजरिवल उन्होंने कभी भी वीपी सिंह का नाम तक लेने की कोशिश नहीं की। क्या इससे ये बात साबित नहीं होती की यदि कोई व्यक्ति जातीय विमर्श शुरू कर दे तो हम लोगों में तनाव आ जाता है। वीपी सिंह के सभी अच्छे काम उनके मण्डल कृत्य से खराब हो गए और वीपी सिंह के नाते देवाशीष मीडिया की भूमिका का पर्दाफाश कर सकते थे।
फिर भी पत्रकार देबाशीष मुखर्जी ने वीपी सिंह पर बहुत शिद्दत और मेहनत से काम किया है और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और आशा करते हैं कि उनका यह काम विद्वानों, राजनीतिक विश्लेषकों को वीपी सिंह की वैचारिक धारणाओं और राजनीति के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करेगा ताकि विश्वविद्यालयों में विश्वनाथ प्रताप सिंह की राजनीति के ऊपर शोध (Research on politics of Vishwanath Pratap Singh) हो।
विद्या भूषण रावत
पुस्तक का नाम : द डिसरप्टर: हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया
विध्वंसक : कैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारत को हिलाकर रख दिया ?
लेखक: देबाशीष मुखर्जी
हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया
प्रकाशन का वर्ष: 2021
कुल पृष्ठ : 542
मूल्य : 699