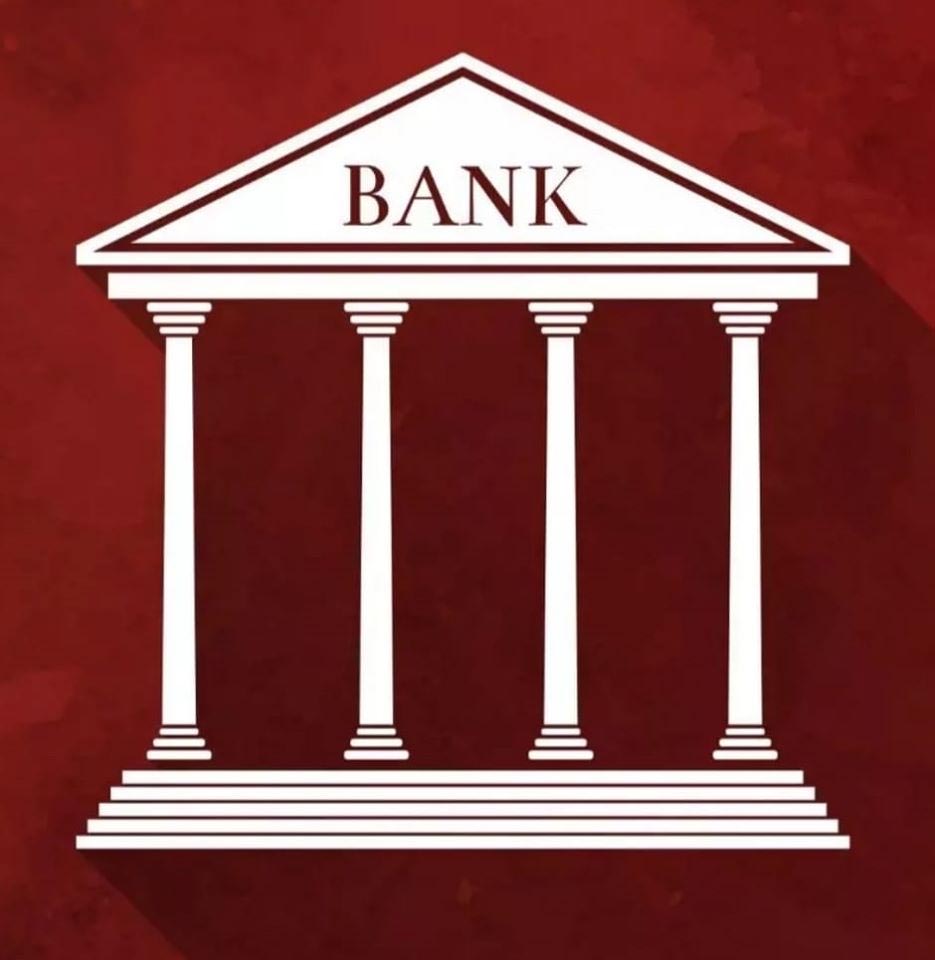German intellectuals appreciate Pramod Ranjan’s article published on Hastakshep
प्रमोद रंजन का यह लेख मूल रूप से हिंदी में था, जिसे उन्होंने "विज्ञान और विशेषज्ञता के आतंक के दौर में बुद्धिजीवियों की ज़िम्मेदारी" शीर्षक से लिखा था। हस्तक्षेप ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। (यहां देखें)
गौरतलब है कि प्रमोद रंजन ने हिन्दी समाज के सांस्कृतिक, वैचारिक और साहित्यिक विमर्श को नए आयाम दिए हैं। वे हिन्दी समाज-साहित्य को देखने-समझने के परम्परागत नज़रिए को चुनौती देनेवाले लोगों में से एक हैं। उनकी किताबों"बहुजन साहित्य की प्रस्तावना" और "बहुजन साहित्येतिहास का
कोविड 19, विज्ञान और बुद्धिजीवियों की ज़िम्मेदारी
- प्रमोद रंजन
लॉकडाउन ने मनुष्यों के शरीरों को ही घरों में नहीं क़ैद किया, बल्कि हम विचारों पर प्रतिबंध के सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। हर मोड़ की ही तरह यहां से भी कई रास्ते अवश्य निकलते हैं। हम कौन-सा रास्ता लेंगे, यह इस पर निर्भर करेगा कि हम कितने समय बाद असल खतरे को भांपते हैं और उस पर प्रतिक्रिया शुरू करते हैं।
इस संघर्ष के अनेक पहलू इस पर निर्भर करेंगे कि हम कितने समय बाद कथित “विशुद्ध” विज्ञान और विशेषज्ञता पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। हमें लोगों को बताना होगा कि विज्ञान, विशेषज्ञता आदि की निष्पक्षता प्रश्नातीत नहीं है।
“हम” से यहां आशय अकादमिशियनों, लेखकों, पत्रकारों व अन्य बुद्धिजीवियों से है। हमारे लिए यह रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि हममें से अधिकांश ने अपने-अपने क्षेत्र की कथित “विशेषज्ञता” का लाभ उठाया है और सवालों को दबाने के लिए गाहे-बगाहे इस हथियार का इस्तेमाल किया है।
कोविड-19 के इस दौर में सरकारों ने विचारों पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, वे एक तरफ हैं। सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अकेले होते तो शायद हम इस कथित महामारी के खत्म होने के बाद इनसे लड़ने और आज़ादी वापस पाने की कोशिश करते। लेकिन अपेक्षाकृत बहुत बड़ा खतरा उस तकनीक से है, जिस पर बिग टेक और गाफा (गूगल, फेसबुक, ट्वीटर, अमेजन आदि) के नाम से जाने जानी वाली कुछ कंपनियों का कब्ज़ा है। बिग टेक द्वारा शुरू की गई यह सेंसरशिप अब तक सरकारों द्वारा लगाई जाने वाली सेंसरशिप से कई गुणा अधिक व्यापक और मजबूत है।
इन कंपनियों की एकाधिकारवादी नीतियों की सफलता और सरकारों की तेजी से बढ़ रही निरंकुशता के बीच का रिश्ता भी साफ तौर पर देखा जा सकता है।
पहले हम सरकारों की निरंकुशता के कुछ उदाहरण देखें।
भारत में कई राज्यों की पुलिस ने कहा है कि “ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोविड -19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकारी मशीनरी द्वारा किए जा रहे काम करने के तरीकों पर संदेह प्रकट करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।” (देखें, ग्रेटर मुंबई पुलिस की आदेश संख्या :CP/XI (06)/Prohibitory order, 23 May, 2020)।
इसी प्रकार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने अपने संकाय सदस्यों को कहा है कि ऐसे किसी विषय पर न लिखें, न बोलें, जिसमें सरकार की किसी भी मौजूदा नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना होती हो। संस्थान ने अपने अध्यापकों को यह छूट दी है कि वे “विशुद्ध” वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलापरक लेखन कर सकते हैं लेकिन उन्हें इस प्रकार का लेखन करते हुए यह ध्यान रखना है कि उनका लेखन किसी भी प्रकार से “प्रशासनिक मामलों को नहीं छुए।”
उपरोक्त दो प्रसंग सिर्फ बानगी के लिए हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुनिया के उन प्रमुख संस्थानों में शुमार हैं, जिसके अध्यापकों को विज्ञान विषयक विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है।
भारत समेत, दुनिया के कई देशों में इन दिनों ऐसे प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो आम लोगों के अनुभव-जन्य ज्ञान और विवेक को ही नहीं, कथित विशेषज्ञों (मसलन, आईआईटी के उपरोक्त अध्यापकों) को भी सवाल उठाने से रोक रहे हैं।
इसलिए मुख्य सवाल यह है कि किसके पक्ष का विज्ञान, किसके पक्ष की विशेषज्ञता, किसके पक्ष की पत्रकारिता को रोका जा रहा है ? ईश्वर और धर्म की ही तरह विज्ञान और विशेषज्ञता की निष्पक्षता पर सिर्फ वही भरोसा कर सकते हैं, जो या तो उससे लाभान्वित हो रहे हों, या फिर मूर्ख अथवा तोतारटंत हों।
भारत प्रेस-फ्रीडम के सूचकांक पर बहुत नीचे रहा है। दुनिया के कुल 180 देशों में इसका स्थान 142वां है। कोविड-19 के दौरान यहां पत्रकारों को सरकारी अमले की नीतियों पर सवाल उठाने तथा कथित तौर पर फाल्स न्यूज फैलाने के आरोप में प्रताड़ित किया जा रहा है।
सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अधिकांश समाचार-माध्यम, जिनमें प्रमुख अखबार, टीवी चैनल, बेवसाइटें, साेशल-मीडिया प्लेटफार्म आदि शामिल हैं; जनता के सवालों के उत्तर के लिए कथित विशेषज्ञ संस्था विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और अमेरिका की “सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन” (सी.डी.सी.) जैसी संस्थाओं की ओर भेज रही हैं। वह भी तब, जबकि ये संस्थाएं खुद ही प्रश्नों के घेरे में रही हैं और इनकी विश्वसनीयता बहुत निचले स्तर की है। इन संस्थाओं पर दवा कंपनियों और परोपकार-व्यवसायियों से साठगांठ, और तीसरी दुनिया के देशों पर कानूनों का उल्लंघन कर घातक दवाओं और वैकसीनों का ट्रायल करने तथा असफल तकनीकों और दवाओं को इन देशों पर थोपने के आरोप अनेकानेक बार साबित हुए हैं।
सवालों को कुचलने का ऐसा क्रूर विश्वव्यापी अभियान मानव-इतिहास में कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के सवालों के उत्तर कभी भी इतने एकआयामी नहीं हुए थे। न ही कभी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर एक साथ कथित विशेषज्ञता इस प्रकार कहर बनकर टूटी थी।
इन संस्थाओं के निर्देशों की आड़ में दुनिया के अनेक विकासशील और गरीब देशों ने अपने देश में कार्यरत मीडिया संस्थानों के लिए ऐसे नियम बनाए हैं, जिसके तहत उन्हें कोविड-19 के संबंध में सिर्फ उन्हीं तथ्यों और रणनीतियों को जनता के सामने रखने की छूट है, जिन्हें इन संस्थाओं की मान्यता प्राप्त हो।
इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इस बीच इन संस्थाओं से इतर मत रखने के कारण सैकड़ों पत्रकारों और समाचार-माध्यमों को प्रताड़ित किया गया है। इनमें आपराधिक मुकदमा, जनता और पुलिस द्वारा पिटाई, आधिकारिक प्रेस कांफ्रेंसों में भाग पर प्रतिबंध, यात्राओं पर प्रतिबंध, प्रेस पास व मान्यता का रद्द किया जाना शामिल है। इस बीच, इन देशों की सरकारों ने कोविड-19 से संबंधित सवाल उठाने पर सैंकड़ों पत्र-पत्रिकाओं को बंद करवाया है, वेबासाइटों को अवरुद्ध कर दिया है तथा प्रकाशित सामग्री को हटाने के लिए मजबूर किया है।
इन प्रताड़नाओं से अधिक चिंताजनक यह है कि एशिया, लातिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में कोरोना वायरस के बहाने सवालों को कुचलने वाले कानून पास कर दिए गए हैं। इस मामले में सबसे बुरी हालत एशियाई देशों में है।
रूसी संसद ने कोविड-19 से संंबंधित सवालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए गत 31 मार्च को अपराध-संहिता में परिवर्तन किया। रूस में अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के बारे में कथित तौर पर गलत जानकारी देता है तो उसे 23000 यूरो (लगभग 19.5 लाख रूपए) तक का जुर्माना और पांच साल तक की जेल हो सकती है और... अगर कोई मीडिया संस्थान ऐसा करता है तो उसे 117,000 यूरो (लगभग 90 लाख रूपए) तक का जुर्माना हो सकता है।
उज़्बेकिस्तान में अप्रैल के पहले सप्ताह में इसके लिए कानूनों में बदलाव किया गया है। नए कानून में आपत्तिजनक सामग्री का भंडारण या प्रबंधन करने पर 8.2 करोड़ उज़्बेकिस्तानी सोम (लगभग 7 लाख् रूपए) का दंड या तीन साल का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति उसे ‘शेयर’ करता है तो उसे 5 साल तक की सजा होगी।
दक्षिण पूर्व एशियाई देश वियतनाम में फरवरी में बने नए कानून के अनुसार अब वहां सोशल मीडिया पर कथित भ्रामक जानकारी देने, शेयर करने पर 10 से 20 लाख डोंग (32 से 64 हजार रूपए) के ज़ुर्माना का प्रावधान किया गया है। यह रकम कितनी ज्यादा है इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यह अधिकांश वियतनामियों के 3 से 6 महीने के मूल वेतन के बराबर है, जो उन्हें महामारी के बारे में कोई “गलत” सवाल उठाने पर चुकानी होगी।
फ़िलीपीन्स कांग्रेस ने 24 मार्च को एक विशेष सत्र आयोजित कर एक कानून पारित किया, जिसमें राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते को कोविड-19 से लड़ने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गईं। नए कानून में सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्मों पर “कोविड-19 संकट के बारे में झूठी जानकारी फैलाने पर दो महीने की जेल और 19,500 डालर (लगभग 14.5 लाख रूपए) का प्रावधान किया गया है। इस अधिकार के मिलने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में दुतेर्ते ने पुलिस और सेना को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। इस दौरान फ़िलीपीन्स से दो बुर्जग लोगों को पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिए जाने की खबरें आईं। फ़िलीपीन्स की जनता की क्या हालत होगी, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के खुद ड्रग-एडिक्ट होने की ख़बरें सामने आती रही हैं। त्रासद यह है कि उन्होंने कुछ साल पहले देश से ड्रग्स के सफाए का अभियान शुरू किया है, जिसमें अब तक पुलिस के हाथों 6 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। दिसंबर, 2016 में राष्ट्रपति ने बी.बी.सी. से एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था, कि उन्होंने कुछ साल पहले डावाओ शहर का मेयर रहते हुए बलात्कार और लूट के तीन आरोपियों की खुद अपने हाथों से हत्या की थी। उन्हाेंने बीबीसी से एक बातचीत में कहा था कि उन्होंने उनके शरीर में कितनी गोलियां मारीं, उन्हें खुद भी इसकी याद नहीं है।
बताने की आवश्यकता नहीं कि क्रूर मनोरोगी सिर्फ फिलीपींस में ही सत्ता में नहीं हैं ! वे अनेकानेक जगहों पर विभिन्न रूपों में मौजूद हैं और देश-समाज की किस्मत लिख रहे हैं।
अज़रबैजान, बोस्निया, कम्बोडिया, जॉर्डन, रोमानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब, ब्राजील, अल्जीरिया, बोलीविया, हंगरी आदि देशों में भी इसी प्रकार के नए कानून बनाए गए हैं।
भारत में इस प्रकार का कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन यहां सरकार, न्यायपालिका और मीडियाहाउसों के मालिक सवालों को दबाने के लिए एकजुट हो गए हैं। उनकी इस एकजुटता ने अभिव्यक्ति की आजादी को अन्य देशों की तुलना में अधिक कहीं अधिक सीमित कर दिया है।
भारत में मीडिया-मालिकों के हित कई अन्य देशों की अपेक्षा सरकारी खज़ाने से बहुत अधिक नाभि-नालबद्ध हैं। यह निर्भरता विज्ञापन के लिए भी है, और मीडिया मालिकों के अन्य व्यवसायों के लिए पर्दे के पीछे से ली जाने वाली अन्य वैध-अवैध रियायतों के लिए भी।
भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के प्रथम लाॅकडाउन की घोषणा 24 मार्च की शाम को की थी। लेकिन इस घोषणा से कुछ घंटे पहले उन्होंने देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों के मालिकों और संपादकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की। इस बातचीत में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, द हिंदू ग्रुप, पंजाब केसरी ग्रुप समेत 11 अख़बारों के 20 प्रतिनिधि शामिल थे। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की गई है, न ही इसमें शामिल हुए अखबारों ने इसमें हुई बातचीत के बारे में अपने पाठकों को कोई जानकारी दी है। इस बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर एक संक्षिप्त सूचना दी गई है। उसके अनुसार, इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान “मीडिया, सरकार और जनता के बीच, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर की एक कड़ी की भूमिका निभाए तथा निरंतर अपना फीडबैक दें”। प्रधानमंत्री ने “जोर दिया कि” इस दौरान “निराशावाद, नकारात्मकता और अफवाह फैलाने वालों से निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है”। उन्होंने अखबारों के मालिकों और संपादकों को कहा कि वे “नागरिकों को आश्वस्त करें” कि “सरकार कोविड -19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है।” आश्चर्यजनक यह था कि उन्होंने समाचार-पत्रों के मालिकों को कोविड-19 से सम्बंधित लेखों और शोध-सामग्री के प्रकाशन के संबंध में भी निर्देश दिए। सामान्य तौर पर सरकारें “खबरों” को ही मन-मुताबिक ढालने तक सीमित रहती हैं। इस कारण लंबे लेखों, पुस्तकों में आने वाला “विचार” पक्ष सेंसरशिप से अपेक्षाकृत बचा रहता है। लेकिन अचानक बुलाई गई इस व्यक्तिगत बातचीत की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाचार-पत्र “अपने पृष्ठों पर प्रकाशित लेखों के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाएं” तथा “अन्य देशों के शोधपत्र व अंतराष्ट्रीय डेटा को शामिल करते हुए वारयस के फैलाव के प्रभावों को उजागर करें”। उनका संकेत डब्ल्यू.एच.ओ., सी.डी.सी. आदि द्वारा वायरस के प्रसार के बारे में प्रसारित किए जा रहे अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ों और महामारी से निपटने के लिए सुझाई जा रही निरंकुश नीतियों को वैधता प्रदान करने की ओर था।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के मालिकों के साथ भी अलग से ऐसी कोई बैठक की या नहीं, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमने देखा कि भारत में संपूर्ण मीडिया सरकार की कोविड-19 संबंधी नीतियों के आगे नतमस्तक रहा। मीडिया के अधिकांश हिस्से ने यहां दुनिया के सबसे सख्त और अमानवीय लॉकडाउन पर कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि लॉकडाउन को कथित तौर पर तोड़ने वाले भूख और बदहाली से बिलबिलाते कमजोर तबकों को समाज और देश के अपराधी के रूप में पेश किया! इस बीच मीडिया का सबसे प्रिय पद “लॉकडाउन/सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियाँ” था। उन्हें इसका भी ख्याल नहीं था कि इस पद को कहते हुए वे समाज के कमजोर तबक़ों के मानवाधिकारों और अपने उन करूण भावों को तार-तार कर रहे हैं, जिनके बूते वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनते हैं।
भारतीय मीडिया के एक बहुत छोटे-से हिस्से ने कमजोर तबक़ों के प्रति करूणा दिखाई तथा एक छोटे-से ही हिस्से ने सरकारी कामकाज में अराजकता और भ्रष्टाचार के सवालों को उठाया। लेकिन इस हिस्से ने भी कोविड-19 की गंभीरता के अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार और इससे निपटने के अमानवीय और बर्बर तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठाया। वे कथित विशेषज्ञता और विज्ञान के पक्ष में पूरी ताकत के साथ खड़े रहे।
इसके बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह "न्याय के बड़े हित" को देखते हुए मीडिया संस्थानों, विशेष कर वेब पोर्टलों को निर्देश दे कि वे कोविड-19 के संबंध में सिर्फ सरकार द्वारा निर्देशित आधिकारिक स्रोतों से ली गई सूचनाएं प्रसारित करें। इस पर कोर्ट ने डब्लूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉ ट्रेडॉस को उद्धृत करते हुए अपने आदेश में कहा कि “हम सिर्फ महामारी से नहीं लड़ रहे, हम इंफोडेमिक ( कथित गलत सूचनाओं के प्रसार)से भी लड़ रहे हैं। फे़क न्यूज़ इस वायरस की तुलना में अधिक तेजी और अधिक आसानी से फैलता है और यह वायरस के जितना ही खतरनाक है” कोर्ट ने कहा कि “हम महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन मीडिया को घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक बातों का ही संदर्भ देने और प्रकाशित करने का निर्देश देते हैं।” इसके बाद सरकार के अलग-अलग प्राधिकारों द्वारा मीडिया को निर्देश जारी किया गया कि उन्हें किन-किन स्रोतों से समाचार संग्रहीत करना है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारिता को सरकार के निर्देशों पर चलने का निर्देश दिया, लेकिन यह आश्चर्यजनक था कि भारतीय अखबारों ने इसे अपनी “जीत” मानते हुए खबरें प्रकाशित कीं कि कोर्ट ने सरकार के आग्रह को खारिज कर दिया है। भारत में समाचार माध्यमों ने किस प्रकार लंबे समय से चली आ रही सेंसरशिप के प्रति अनन्य स्वीकार-भाव विकसित कर लिया है, उसका यह एक रोचक उदाहरण है। कोर्ट के फैसले को अपनी “जीत” बता कर वे न सिर्फ सेंसरशिप का विरोध करने की जहमत उठाने से बच गए बल्कि अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता का झूठा ढिंढोरा पीट कर अपनी पीठ थपथपा डाली।
लेकिन कहना मुश्किल है कि क्या कोविड के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया की चुप्पी का कारण सिर्फ प्रधानमंत्री का भय, अखबार मालिकों के सरकार से जुड़े आर्थिक हित हैं, या न्यायालय का निर्देश है। इन चीजों ने निश्चय ही निर्णायक भूमिका निभाई, लेकिन यह भी सच है अधिकांश पत्रकार स्वयं भी कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों के पूर्वानुमान और इटली और अमेरिका से आई मौतों की संख्या से आक्रांत हैं। उनमें से अधिकांश को आज भी यह जानकारी नहीं है कि वे पूर्वानुमान फर्जी साबित हो चुके हैं तथा इम्पीरियल कॉलेज के नील फर्गुसन से ब्रिटेन के सांसद पूछताछ कर रहे हैं। इसी प्रकार, उन्हें यह भी मालूम नहीं है मौतों के आंकड़ों के संकलन के लिए ऐसी पद्धति अपनाई जा रही है, जो भले ही चिकित्सा विज्ञान के शोध के लिए उचित हो, लेकिन उससे जो आंकड़े पैदा हो रहे हैं, वे अतिशयोक्ति-पूर्ण हैं। इसका मुख्य कारण है कि अधिकांश लोगों की ही तरह मीडिया में कार्यरत लोगों की तथ्यों तक पहुंच बहुत कठिन बना दी गई है।
दरअसल, बिग टेक की नीतियों का प्रभाव उनके अपने प्लेटफार्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पत्रकारों और लेखकों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले सूचनाओं के स्रोतों पर भी असर डाल रहा है। बिग टेक ने महामारी से पहले और महामारी के दौरान, जो नीतियाँ बनाई, उसके तहत वे विरोध में जाने वाले कुछ सूचनाओं के स्रोतों को नष्ट कर दे रहे हैं जबकि अधिकांश तक लोगों की पहुंच लगभग असंभव बना रहे हैं।
इसके अतिरिक्त बिग टेक कथित “फैक्ट चेकिंग” संस्थाओं को धन मुहैया करवा कर विरोधी स्रोतों को अविश्वसनीय बनाने का अभियान चला रही हैं। साथ ही, छोटे ब्लॉगों, वेबसाइटों व अन्य वैकल्पिक व मुख्यधारा के समाचार-माध्यमों को धन उपलब्ध करवा कर फैक्ट चेकिंग संस्थाओं में तब्दील कर रही हैं। इन काम के लिए सिर्फ ये टेक जायंट्स ही नहीं, बल्कि परोपकार-व्यवसायी व कई अन्य वैश्विक संस्थाएं भी पिछले कुछ वर्षों से धन उपलब्ध करवा रही हैं। इनमें मुख्य है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फ़ाउंडेशन। कोविड-19 से कुछ समय पहले ही उन्होंने इस दिशा में थैलियां खोल दी थीं, कोविड-19 के बाद उन्होंने इसका मुंह और चौड़ा कर दिया है। (इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए मेरा एक अन्य लेख यहां देखें)
बहरहाल, पत्रकारिता विधा की अपनी संरचनागत सीमाएं हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उन सीमाओं के भीतर रहकर निभाए जा सकने वाले कर्तव्यों को भी पूरा करने में पत्रकारिता विफल रही है। उसके कारणों में यहां जाने का अवकाश नहीं है। यहां इतना याद दिला देना पर्याप्त होगा कि अगर पत्रकारिता इस कथित महामारी के संदर्भ में सिर्फ एक तुलना भी प्रस्तुत कर पाती तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती। यह तुलना कुछ यों हो सकती थी कि आज दुनिया में अन्य संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों से कितने लोग मरते हैं और लॉकडाउन की वजह से इसमें कितना इज़ाफा होने की संभावना है।
किताबों पर बिग टेक के प्रतिबंध के मायने
पत्रकारिता के साथ इस दौर में जो हुआ, उसे संक्षेप में देख लेने के बाद अब हम न्यूयॉर्क टाइम्स में “व्यापार संबंधी खोजी पत्रकार” के रूप में काम कर चुके एलेक्स बेरेनसन की किताब के प्रसंग को देखें।
बेरेनसन ने अपनी किताब किताब “कोविड- 19 और लॉकडाउनों से संबंधित अनकही सच्चाइयाँ”, भाग - 1 (Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns) में विभिन्न सरकारों और स्वास्थ्य-संस्थाओं द्वारा जारी उन तथ्यों को रखा है, जिन्हें किसी रहस्यमय कारण से समाचार माध्यमों में जगह नहीं मिल रही है। उन तथ्यों से उजागर होता है कि कोविड-19 की भयावहता उससे बहुत कम है, जितना कि इसे प्रसारित किया गया है। (किताब का प्रथम 1000 शब्द लेखक की वेबसाइट पर यहां पढें : http://www.alexberenson.com/the-first-1000-words-of-chapter-1-of-unreported-truths-about-covid-19-and-lockdowns-the-booklet-amazon-has-censored/ )
अमेजन ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया था।
बेरेनसन ने न्यूयार्क टाइम्स में इराक के कब्ज़े के लिए हुए युद्ध और खतरनाक दवाओं से संबंधित उद्योगों को भी कवर किया था। वर्ष 2010 में न्यूर्याक टाइम्स को विदा कहने के बाद वे उपन्यास लेखन की ओर मुड़ गए। उनके उपन्यास आम पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। 2007 में उनका एक उपन्यास न्यर्याक टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी शामिल रहा था। उपन्यासों की उनकी “जॉन वेल्स सीरिज़” के उपन्यासों की दुनिया भर में 10 लाख से अधिक प्रतियाँ बिकीं। इनमें ज्यादातर ईबुक्स थीं।
बेरेनसन खुद को “अमेजन-राइटर” ">कहते हैं। दरअसल, उनकी किताबों की सबसे अधिक बिक्री अमेजन के ईबुक स्टोर किंडल से होती रही है। किताबों के प्रकाशन की इस नई और बेहद सस्ती तकनीक ने उनके जैसे साहित्यिक दुनिया में लंबे समय तक दखल नहीं रखने वाले, अनेकानेक लेखकों को उड़ान के लिए नया आसमान दिया है।
2019 में ईबुक का वैश्विक मार्केट शेयर (बिक्री से होने वाली आय) कुल किताबों की बिक्री का 18 प्रतिशत था, जबकि संख्या के हिसाब से कुल बिकी किताबों में से 36 प्रतिशत ई-बुक्स थीं। आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली अलग-अलग संस्थाओं के अनुसार ई-बुक्स में से 67 से 83 प्रतिशत का शेयर अकेले अमेजन (किंडल) का था।
2019 में ई-पुस्तकों का बाजार 18.13 बिलियन अमरीकी डॉलर था, 2025 तक इसके 23.12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। वह भी तब जब दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी के बढ़ने और मध्यवर्ग की क्रय शक्ति में भारी कमी होने की उम्मीद है।
ईबुक्स के बाजार में तेज बढ़ोत्तरी का कारण इलेक्ट्रॉनिक किताबों को पढ़ने वाले उपकरणों का उन्नत होते जाना और किताबों व अन्य दस्तावेज़ों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया का तेज होना है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आम पाठक ही ईबुक्स और ऑडियो बुक्स की ओर नहीं आए, बल्कि विश्वविद्यालयों, स्कूल व अन्य संस्थाएं भी अपने पुस्तकालयों में इन्हें शामिल करने के लिए विवश हुईं हैं।
ई-बुक्स के अतिरिक्त प्रिंट किताबों के बाजार पर भी ई-कॉमर्स का क़ब्ज़ा होता गया है। किताबों की दुकानें दिनों-दिन बंद होती जा रही हैं। इस क्षेत्र में भी अमेजन का ही एकाधिकार है।
इन आँकड़ों को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम समझ सकें कि अमेज़न द्वारा किताबों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध का असर क्या हो सकता है।
एलेक्स बेरेनसन ने अपनी किताब 4 जून, 2020 को ईबुक के रूप में अमेजन पर प्रकाशित की थी। अमेज़न पर जारी होते ही बड़ी संख्या में लोगों ने इसे खरीदा, लेकिन जल्दी ही अमेजन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। बेरेनसन को भेजे गए एक ईमेल में अमेजन ने बताया कि उनकी किताब अमेजन के कंटेंट संबंधी नियमों का उल्लंघन करती है, इसलिए उसे हटा दिया गया है।
बेरेनसन ने अमेजन के मेल का उत्तर दिया, लेकिन जैसा कि अमेज़न ऐसे मामलों में करता है, उन्हें अमेज़न की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला।
हताश बेरेनसन ने इस बारे में अपने ट्विटर पर लिखा, जिस पर एलन मस्क की नजर पड़ी।
मस्क दुनिया की दो प्रभावशाली कंपनियों - स्पेसएक्स (अंतरिक्ष परिवहन से संबंधित) और टेस्ला (इलेक्ट्रिक कार और सौर उर्जा से संबंधित) के संस्थापक और सीईओ हैं। उनकी कंपनियों के लक्ष्यों में टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी की स्थापना करना शामिल है। टेस्ला या स्पेसएक्स की अमेजन के साथ सीधी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं रही है लेकिन मस्क और बेजोस अंतरिक्ष उद्योग में लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी हैं।
जिस समय बेरेनसन इस किताब को लिख रहे थे, उस समय में उन्होंने अपने अध्ययन का एक अंश ट्वीट किया था, जिसे एलन मस्क ने अपने एकाउंट पर री-ट्वीट किया था।
मस्क आरंभ से ही लॉकडाउन के विरोधी रहे हैं। कुछ मीडिया-रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को जारी रखने पर बल देते हुए कर्मचारियों को कहा था कि “कोविड-19 से मौत का उतना ही खतरा है, जितना की किसी दुर्योगपूर्ण कार-एक्सीडेंट से मरने का।”
अमेज़न द्वारा बेरेनसन की इस किताब को बैन करने की सूचना से तिल मिलाए मस्क ने तुरंत अमेज़न के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा “अमेज़न को तोड़ देने का समय आ गया है, एकाधिकार गलत है”।
इसके बाद अमेज़न हरकत में आया और लेखक को मेल करके बताया कि उनकी किताब अमेज़न पर फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके बाद से दो सप्ताह बीत जाने के बावजूद यह किताब दुनिया के बड़े-बड़े लेखकों को पछाड़ते हुए अमेजन पर बेस्ट सेलर बनी हुई है। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। न सिर्फ बेस्ट सेलर बनी हुई है, बल्कि उनके द्वारा किताब में दिए गए तथ्यों का कोई खंडन अभी तक किसी संस्था अथवा विशेषज्ञ की ओर से नहीं आया है।
लेकिन दुनिया के एक अमीर ने दूसरे अमीर के समक्ष अगर इस किताब को प्रतिबंधित करने का विरोध नहीं किया होता, तो क्या होता? तब हम शायद इस किताब के अस्तित्व से भी अपरिचित होते।
ई-बुक्स/ऑडियो बुक्स का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, उसका एक तकनीकी पहलू यह भी है कि अगर ये कंपनियां चाहें तो ग्राहकों द्वारा खरीदी गई किसी भी किताब को उनकी लाइब्ररेरी से हटा सकती हैं। वे ऐसा करती भी रही हैं। प्रिंट किताबों के परंपरागत बाजार में ऐसा नहीं था।
डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल करेंसी के खतरों को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस अर्थव्यवस्था में आम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, जिसे वे दबा कर रख सकें। वह आभासी आर्थिक दुनिया उंगलियों पर गिने जा सकने वाले पूंजीपतियों के पास धन के केंद्रीकरण को इतना बढ़ा देगी कि राष्ट्रों की प्रभुसत्ता निरर्थक होने लगेगी।
विज्ञान और धर्म
काेविड-19 से संबंधित तथ्यों को लेकर, जिस प्रकार के असमंजस की स्थिति सयास पैदा की गई है, उससे हममें से कई किम्कर्तव्यविमूढ हैं। हमें मीडिया और अपनी सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों के माध्यम से प्रचारित करवाए जा रहे अनेक तथ्यों पर संदेह हो रहा है, लेकिन हम प्राय: उन्हें सार्वजनिक मंचों पर रखने में संकोच महसूस कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमने अकादमिक विशेषज्ञता को सहज-विवेक और अनुभवजन्य ज्ञान के साथ अन्योन्याश्रित रूप से विकसित करने के लिए कोई संघर्ष नहीं किया है। हम भूल चुके हैं कि विवेक को खरीदा नहीं जा सकता और अनुभव की प्रमाणिकता को खंडित नहीं किया जा सकता, जबकि विशेषज्ञता अपने मूल रूप में ही बिकाऊ होती है और कथित विशुद्ध विज्ञान मनुष्यता के लिए निरर्थक ही नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक साबित हाे रहा है।
2007 का एक प्रसंग याद आता है। यह प्रसंग इसलिए अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि इसका एक पक्ष कोविड के भय को अपनी कथित मॉडलिंग से अनुपातहीन बनाने वाले इम्पीरियल कॉलेज से जुडा है, जबकि दूसरे का नाम कोविड के दौर में अपने शोध-पत्रों के लिए बार-बार समाचार-पत्रों में आ रहा है।
इम्पीरियल कॉलेज, लंदन के प्रोफेसर डेविड किंग उन दिनों ब्रिटेन की सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। वे उन दिनों आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्यान्न (GM foods) को बिट्रेन सरकार द्वारा स्वीकृत करवाने के लिए प्रयासरत थे। जबकि बिट्रेन में अनेक लोग इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों कहना था कि वे अपने अनुभव से यह महसूस कर सकते हैं कि खाद्यान में किया गया अनुवांशिक फेरबदल न सिर्फ उनके स्वास्थ पर बुरा असर डाल रहा है बल्कि यह पर्यावरण और जैव-विविधता के लिए भी खतरनाक है। जबकि किंग का कहना था कि विज्ञान से यह प्रमाणित हो चुका है कि जीएम खाद्यान्न, गैर-जीएम प्राकृतिक खाद्यान्न के तुलना में अधिक सुरक्षित हैं तथा जीएम तकनीक ने दुनिया की बढती आबादी का पेट भरने का एक सफल तरीका पेश किया है।
बिट्रेन के पत्रकारों ने जब लोगों की चिंताओं को उठाया तो डेविड किंग बिफर गए। उन्होंने “विज्ञान” पर सवाल उठाने के लिए मीडिया संस्थानों को खरी-खोटी सुनाई। उनका कहना था कि “विज्ञान किसी भी समाज के
मेडिकल साईंस की दुनिया की सबसे पुरानी और प्रमुख पत्रिका द लान्सेन्ट के प्रधान संपादक रिचर्ड होर्टन ने द गार्डियन के 11 दिसंबर, 2007 अंक में इस प्रसंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डेविड किंग की आलोचना की थी। रिचर्ड होर्टन ने उस समय जो कहा था, वह आज अधिक प्रासंगिक है। होर्टन ने लिखा था कि डेविड किंग को एकपक्षीय, सर्वसत्तात्मक नजिरए से विज्ञान को नहीं देखना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि “विज्ञान प्रयोगों और समीकरणों की किसी अमूर्त दुनिया में मौजूद नहीं है। विज्ञान लोकतांत्रिक बहस की अराजकता का हिस्सा है।”
हमने बाद में भारत के अनुभव से भी पाया कि जीएम खाद्यान्न किस प्रकार खाने वालों के स्वास्थ के लिए और पर्यावरण व जैव विविधता के लिए तो खतरा हैं ही। वे किसानों को भी बर्बाद कर देते हैं। पिछले वर्षों में भारत में हजारों किसान बीटी कॉटन बीजों के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। भारत व अन्य देशों में जीएम खाद्यान्न के दुष्प्रभावों के कारण इनके उत्पादन पर प्रतिबंध है। ब्रिटेन में भी सरकार ने प्रोफेसर किंग की बात नहीं मानी। वहां भी जीएम खाद्यान्न आज तक प्रतिबंधित है।
“विज्ञान " ज्ञान के सतत विकास का एक चरण है। या कहें कि आज उपलब्ध ज्ञान के घनीभूत रूप का एक नाम है। यह एक तरह से ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। बहसों और विमर्शों से ही सुंदर, कल्याणकारी विज्ञान का विकास हो सकता है।
विज्ञान का जन्म और विकास भी वैसे ही हुआ है, जैसे कभी धर्म का हुआ था। धर्म भी अपने समय में उपलब्ध सर्वोत्तम ज्ञान का घनीभूत रूप था। वह भी अपने समय के ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष था। समस्या तब पैदा होती है, जब इनका प्रयोग शक्तिशाली तबका अपना हित साधने के लिए करने लगता है। यही धर्म के साथ हुआ था, यही आज विज्ञान के साथ हो रहा है।
दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग व संस्थाएं विज्ञान की नई-नई खोजों के सहारे मनुष्य जाति को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। कोविड के भय को अनुपातहीन बनाने में भी इन्हीं से संबद्ध संस्थाओं की भागीदारी सामने आ रही है।
धर्म या विज्ञान के समर्थन और विरोध का सवाल नहीं है। ऐसा कौन होगा, जो खुद को अधार्मिक कहना चाहेगा, ऐसा कौन होगा, जो स्वयं को अवैज्ञानिक कहना चाहेगा।
लेकिन हम पंडा-पुरोहित, सामंतों-राजाओं से धर्म की मुक्ति के लिए लडे हैं और हममें से कुछ ने नास्तिक कहलाने का खतरा उठाया है। कुछ ने धर्म ने पीछा छुडाने के लिए खुद को “सत्य का खोजी” तो कुछ ने आध्यात्मिक कहना पसंद किया।
कुछ लोग धर्म और अंधविश्वासों में विज्ञान की तलाश करते हैं। मसलन, कुछ लोग कोविड का इलाज गौमूत्र में तलाश रहे थे। यह मूर्खता हो सकती है, और इस तरह की हरकतों के मानवद्वेषी निहितार्थ भी होते हैं। लेकिन धर्म में विज्ञान की तलाश करना उतना बुरा नहीं है, जितना कि विज्ञान को धर्म बनाने की कोशिश करना। आप देखेंगे, जो लोग गौमूत्र से कोविड का इलाज ढूंढ रहे थे, वे ही लॉकडाउन के दौरान सडकों पर डंडा लेकर सबसे पहले “विज्ञान” का पालन करवाने निकले थे।
जैसे धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही आज विज्ञान का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है।
मेरे एक संपादक मित्र ने कहा कि वे विज्ञान पर आस्था रखते हैं। मैंने उन्हें कहना चाहता हूं कि आस्था से अधिक अवैज्ञानिक चीज कोई और नहीं है। हम विज्ञान की ओर इसलिए आए थे कि यह हमें विवेक और तर्क पर आधारित सत्य की खोज के लिए प्रेरित करेगा। अगर विज्ञान से हम आस्था ग्रहण कर रहे हैं, तो जरूर कोई भारी गड़बड़ है।
मनुष्यता की रक्षा के लिए हमें विज्ञान की मुक्ति के लिए संघर्ष छेड़ना चाहिए। खुद को विशुद्ध वैज्ञानिक सोच का कहना, कट्टर धार्मिक कहने के समान है। आज जब विज्ञान धर्म बनने लगा है तो हमें दुनिया को सुंदर बनाने के उसके दावों पर संदेह करना ही होगा।
हम सभी को सोचना होगा कि कोविड के बहाने विमर्श और बहसों पर जिस समय रोक लगाई जा रही थी, जिस समय विशेषज्ञता और विज्ञान के नाम पर करोड़ों लोगों को, बेरोज़गारी, भूख और बदहाली की ओर धकेला जा रहा था, उस दौरान हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी, क्या हमने उसे पूरा किया है? अभी भी अवकाश है, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों पूरा करने का इरादा रखते हैं?
< प्रमोद रंजन की दिलचस्पी सबाल्टर्न अध्ययन, आधुनिकता के विकास और ज्ञान के दर्शन में रही है। ‘साहित्येतिहास का बहुजन पक्ष’, ‘बहुजन साहित्य की प्रस्तावना’ और ‘शिमला-डायरी’ उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित दक्षिण भारत के सामाजिक-क्रांतिकारी ईवी रामासामी पेरियार के प्रतिनिधि विचारों पर केंद्रित तीन पुस्तकों का प्रकाशन हाल ही में हुआ है। रंजन इन दिनों असम विश्वविद्यालय के रवींद्रनाथ टैगोर स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज में प्राध्यापक हैं।}