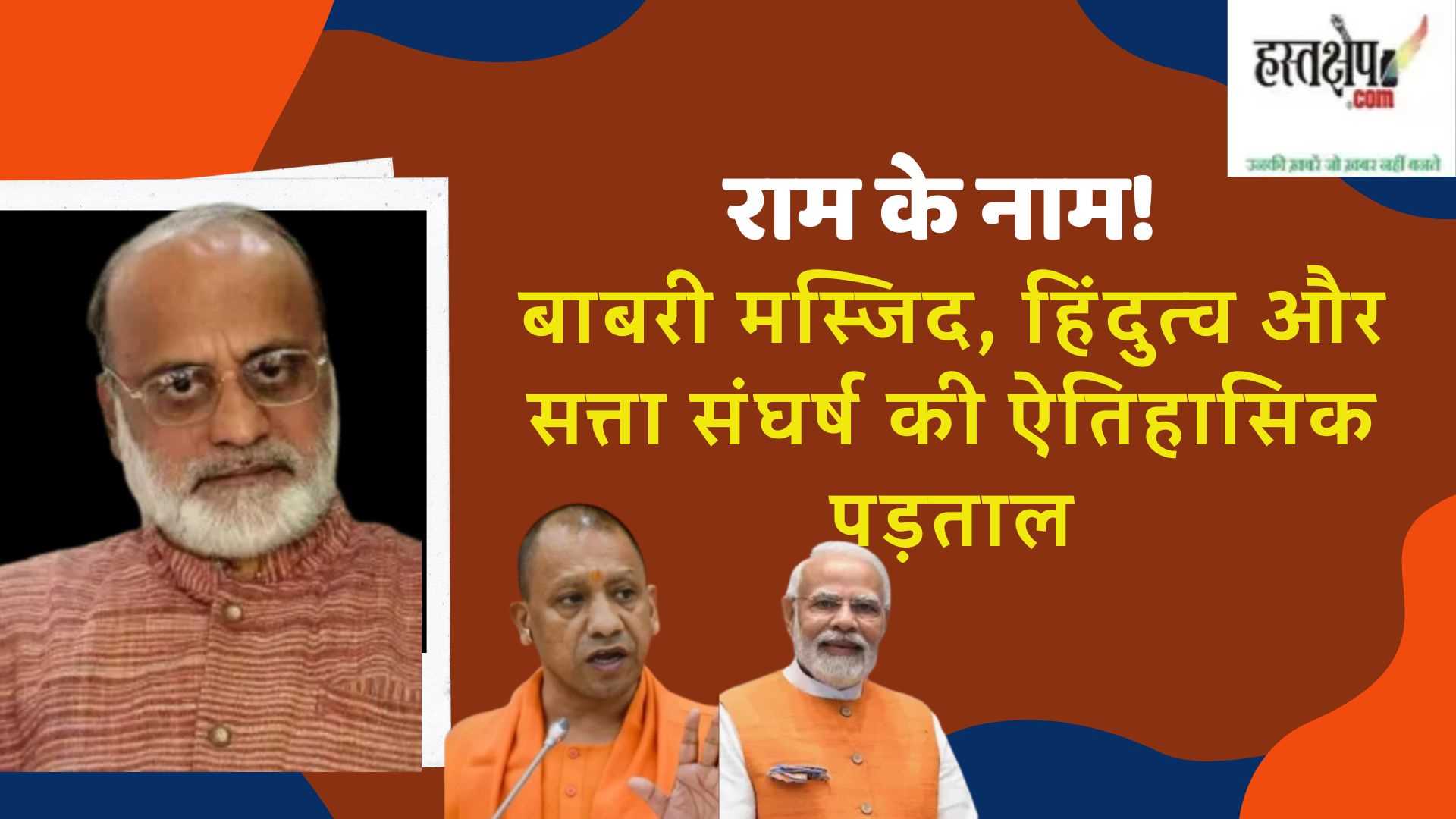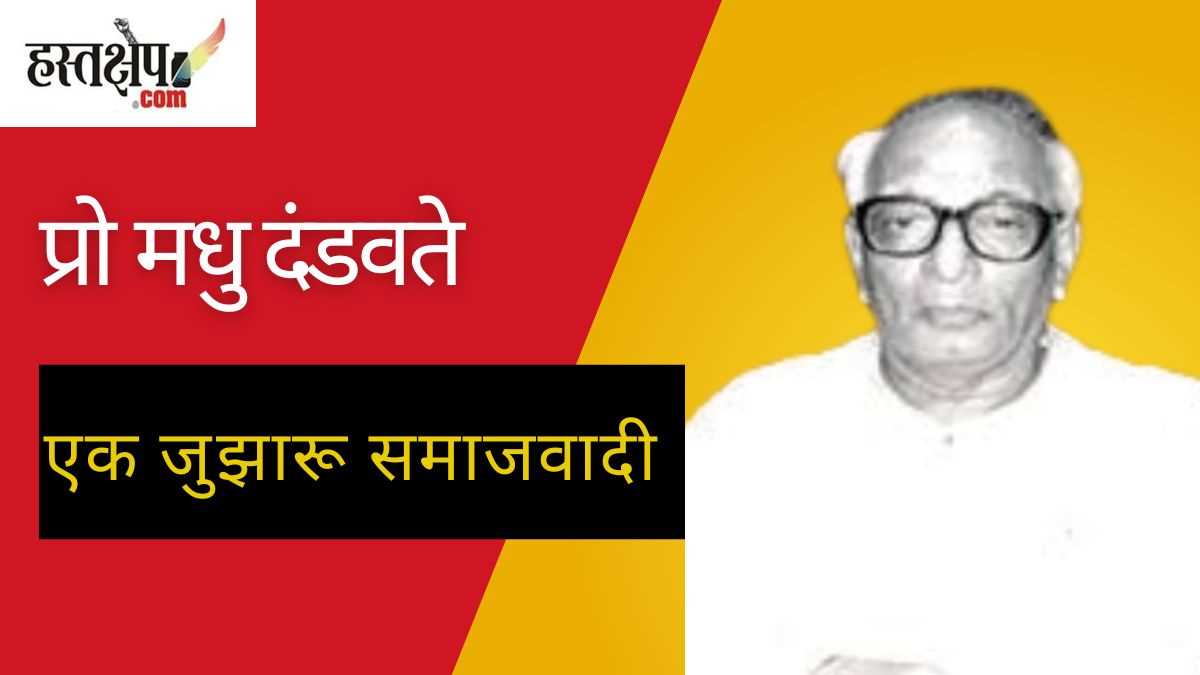Is disability only physical?
- विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विशेष - (International Day of Persons with Disabilities)
अक्सर हमारी विकलांग सोच ही शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के जीवन को कठिन बना देती है। वे अपनी शारीरिक अक्षमता को तो किसी हद तक झेल लेते हैं, परन्तु उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जूझ पाना आसान नहीं होता।
ऐसा मानना है तंज़िला खान का जो विकलांग अधिकारों पर कार्य करने वाली एक जानी मानी कार्यकर्ता हैं और गर्ली-थिंग्स की संस्थापिका हैं.
प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य और अधिकार पर आयोजित एशिया पैसिफिक क्षेत्र के सबसे बड़े अधिवेशन (१०वीं एशिया पैसिफिक कांफ्रेंस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड राइट्स-10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights) के बारहवें वर्चुअल सत्र में तंज़िला ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित अपने विचार साझा करते हुए कहा कि,
"विकलांगों को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम खुद को समाज में फिट नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में, सभी इमारतें केवल शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए ही सुलभ बनायीं जाती हैं। यही बात नीतियों और कानूनों पर भी लागू होती है। कभी-कभी लोगों
एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ६९ करोड़ लोग विकलांगता से ग्रसित हैं. हालांकि कई देशों ने विकलांगों के लिए रोज़गार और शिक्षा की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किये हैं, लेकिन उनके प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य की जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है. महिलाओं के प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य अधिकार कुछ देशों में अभी भी वर्जित विषय हैं और विकलांग महिलाओं के संदर्भ में तो यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है.
प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी सीमित पहुँच का एक बहुत बड़ा कारण है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की असंवेदनशीलता (Insensitivity of healthcare providers).
नेपाल की शिबू श्रेष्ठा जो 'विज़िबल इम्पैक्ट' में कार्यरत हैं, ने बताया कि उनके देश में युवाओं, विशेष रूप से अपंग महिलाओं, को इस सम्बन्ध में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वैसे भी नेपाल में युवा महिलाओं की परिवार नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताएं भारी मात्रा में अपूर्ण हैं. तिस पर यह माना जाता है जो विकलांग हैं वे यौन रूप से सक्रिय नहीं हैं और इसलिए उन्हें प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं की आवश्यकता ही नहीं है.
नेपाल के तीन शहरों में विकलांग युवा व्यक्तियों पर किए गए एक अध्ययन में प्रतिभागियों ने कहा कि युवा विकलांगों को परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का रवैया स्नेहशील और मित्रतापूर्ण नहीं होता है। शिबू ने सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) को बताया कि सेवा प्रदाता अक्सर यह कहते हुए पाये गए कि "क्या इन लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है?"
अध्ययन में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने बताया कि परिवार नियोजन के मुद्दों पर अभी भी खुलकर चर्चा नहीं की जाती है। कदाचित इसीलिए उनमें परिवार नियोजन विधियों के बारे में जानकारी बहुत कम है.
Which method of family planning should be adopted
महिला प्रतिभागियों ने बताया कि विवाहित जोड़ों में पति ही यह तय करता है कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाया जाये। और इस निर्णय में महिलाओं की सहभागिता न के बराबर होती है।
एक महिला प्रतिभागी ने कहा,
"वे (पुरुष) (सम्भोग के) अगले दिन आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली खरीद कर लाने की पेशकश करते हैं और हमें उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है. हममें इतना आत्मविश्वास ही नहीं है कि हम स्वयं बाज़ार से गर्भनिरोधक खरीद सकें। इसलिए हम अक्सर असुरक्षित यौन संबंध (Unprotected sex) बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं."
काठमांडू की एक विकलांग महिला ने कहा,
"एक बार मैं जब 'वैजाइनल टेबलेट' खरीदने गई तो फार्मासिस्ट ने मुझे इस तरह देखा जैसे मैंने कोई हत्या कर दी हो. तब से मैं कभी अपने आप गर्भनिरोधक खरीदने नहीं जाती हूँ."
गर्भनिरोधक के उपयोग से जुड़ी अनेक भ्रांतियां भी विकलांग व्यक्तियों में प्रचलित हैं - जैसे कि 'कॉन्डोम और आईयूडी यौन संतुष्टि नहीं देते हैं', या फिर 'नसबंदी कराने से पुरुष कमज़ोर हो जाता है' जैसी भ्रांतियां.
जब बड़े शहरों में रहने वालों के दृष्टिकोण और समझ का यह स्तर है तो सोचिये छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल होगा।
शिबू चाहती हैं कि विकलांगों के लिए सभी उचित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध हों, जैसे कि 'रैम्प' (इमारत आदि में जीने के साथ-साथ ढलान-वाला रास्ता जिससे कि पहियेदार-कुर्सी पर लोग ऊपर-नीचे आ-जा सकें), शौचालय में 'ग्रैब बार' (हैंडल जिससे कि लोग आसानी से सहारे के साथ उठ सकें), अस्पताल आदि में रोगी को देखने के लिए कम ऊंचाई का बिस्तर, सांकेतिक भाषा व्याख्याकार, ऑडियो प्रारूप, ब्रेल लिपि में पठन सामग्री, आदि.
मुंबई के जनसँख्या शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंस्टिट्यूट में शोधरत स्रेई चंदा द्वारा भारत के दो महानगरों में किए गए अध्ययन से किसी दुर्घटना के कारण हुए निचले अंग विच्छेदन से ग्रसित विकलांग व्यक्तियों की दुर्दशा का पता चलता है.
स्रेई के अनुसार अंग विच्छेदित लोगों को न केवल शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों से जूझना पड़ता है, वरन उनकी यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएं भी काफी हद तक अपूर्ण रह जाती हैं.
घुटने के नीचे से अपंग एक व्यक्ति ने कहा,
"हम सभी बातें अपनी माँ के साथ तो नहीं साझा नहीं कर सकते. कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए दोस्तों की ज़रुरत होती है. मगर विकलांग होने के कारण यौन इच्छा और आवश्यकता के बारे में दोस्तों के साथ भी बात करना मुश्किल हो जाता है."
एक अन्य युवा महिला, जिसके दोनों पाँव घुटने के नीचे से विच्छेदित थे, ने बताया कि जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया. जब वह प्रसूति के लिए अस्पताल गई तो स्वास्थ्यकर्मियों ने कहा, 'आपके पैर नहीं हैं, हम आपका प्रसव करवाने का जोखिम नहीं उठा सकते.'
महिला ने बताया,
"हालांकि मुझे बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई, लेकिन हर किसी से अपने बारे में 'लिबंलेस' (अपंग) जैसे शब्द सुनकर बहुत कष्ट हुआ."
बर्मा में कलरफुल-गर्ल्स की संपादिका फ्यू न्यू विन का कहना है कि उनके देश में विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों, की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताएं काफी अपूर्ण हैं. ऐसा मुख्य रूप से इस गलत धारणा के कारण है कि उनमें यौन इच्छा की कमी होती है और इसलिए उन्हें इन सेवाओं की ज़रुरत नहीं है. इस भ्रान्ति के चलते उन्हें यौन शिक्षा कार्यक्रमों से भी वंचित रखा जाता है. और जब उन्हें अन्य शैक्षिक गतिविधियों में शामिल भी किया जाता है तो उनकी आवश्यकता अनुरूप विशिष्ट सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
Many misconceptions and misinformation related to the reproductive and sexual health of the disabled are prevalent in society.
विकलांगों के प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक भ्रांतियां और गलत जानकारी समाज में व्याप्त हैं, जिनके बहुत से प्रतिकूल प्रभाव विकलांग लड़कियों और महिलाओं को झेलने पड़ते हैं- जैसे कि जबरन शादी, घरेलू और यौन हिंसा, सुरक्षित यौन संबंध पर ज़ोर देने के लिए आत्म शक्ति की कमी जो प्रायः अनपेक्षित गर्भधारण और यौन संचारित संक्रमण को बढ़ावा देती है.
ये कुछ हृदय विदारक ज़मीनी हकीकतें हैं जिनका सामना विकलांग व्यक्तियों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में करना पड़ता है। लेकिन इस अँधेरे में उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं। वियतनाम एक ऐसा देश है जो इस सन्दर्भ में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
Vietnam is very progressive in reproductive and sexual health care
वियतनाम की एन गुयेन ने बताया कि प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य सेवा के मामलों में वियतनाम काफी प्रगतिशील है. अधिकांश लोगों को गर्भनिरोधी उपाय आसानी से उपलब्ध हैं. सरकारी नीतियाँ भी प्रजनन अधिकारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती हैं. हाल ही में लागू किये गए विकलांगता कानून के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कई सकारात्मक कदम उठाये गए हैं.
एन गुयेन द्वारा 'शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए हो ची मिन्ह शहर में प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच' विषय पर किए गए शोध में पाया गया कि इन महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते समय बहुत ही सकारात्मक अनुभव हुआ. प्रतिभागियों ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता उनकी विशेष आवश्यकताओं के बारे में जानकारी रखते हैं और संवेदनशील भी हैं. अस्पतालों और स्वास्थ्य क्लीनिकों में रैंप, लिफ्ट और व्हीलचेयर का प्रावधान है. विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी हैल्थकेयर कार्ड की सुविधा है जिससे उन्हें या तो निःशुल्क या कम शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं.
परन्तु कुछ परेशनियों का भी ज़िक्र हुआ-- जैसे कुछ अस्पतालों में शौचालय व्हीलचेयर सुलभ नहीं हैं, या कहीं पर पार्किंग मुख्य प्रवेश द्वार से बहुत दूर है, या फिर कहीं तीन पहिया मोटरबाइक की पार्किंग की अनुमति नहीं है.
पाकिस्तान में, तंज़िला की 'क्रिएटिव ऐली' नामक ड्रामा/नाट्य प्रोडक्शन कंपनी नीतिगत स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के मुद्दों को उजागर करने के लिए और आम जनता को जागरूक करने के लिए अभिनव तरीकों का उपयोग कर रही है. उनका 'थियेटर ऑफ द टैबू' एक ऐसा प्रशिक्षण मॉड्यूल है जो नाट्य के ज़रिये प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य अधिकारों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है.
तंज़िला ने बताया,
"हमारा थिएटर आम थिएटर जैसा नहीं है। हमारे नाटकों में दर्शक स्वयं अभिनय करने वाले बन जाते हैं. वे स्वयं ही अपने पूर्वाग्रहों को संबोधित करते हैं और समस्या का समाधान ढूँढते है। यह एक बहुत ही सुखद और आनंददायक तकनीक साबित हुई है. हम अपने थिएटर कार्यक्रमों में विकलांगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी शामिल करते हैं ताकि विकलांग अपने को अलग थलग न महसूस करें".
तंज़िला ने 'गर्ली थिंग्स' नामक एक मोबाइल ऍप की भी स्थापना की है, जो सैनिटरी पेड सहित महिलाओं के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता संबंधित उत्पादों की होम डिलीवरी करता है। यह महिलाओं को स्त्री-स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उन उत्पादों तक पहुँच प्रदान करता है जो वे सीधे दुकान से खरीदने में या तो झिझक महसूस करती हैं या फिर अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण अकेले बाज़ार जाने में अक्षम हैं. इस ऍप सेवा के ज़रिये महिलाएं और लड़कियां अपने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सम्बन्धी वस्तुएं खरीदने के लिए किसी अन्य पर नहीं, वरन स्वयं पर निर्भर हैं।
तंज़िला का मानना है कि विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें मुख्य धारा में लाना और उन्हें अपने जैसा ही मानना. हमें उनको अपने दान के लाभार्थी के रूप में नहीं देखना चाहिए. हम सबके साथ समानता का व्यवहार करें और उनमें किसी भी प्रकार की असमर्थता या दुर्बलता होते हुए भी (चाहे वह दुर्बलता शारीरिक हो अथवा उनकी पृष्ठभूमि या जेंडर आइडेंटिटी से सम्बंधित हो) उनके प्रति कोई भी अक्षम रवैया या अपंग सोच न अपनाएं। तभी हम ऐसे विश्व का सपना साकार कर पायेंगें जहाँ कोई भी पीछे नहीं छूट पायेगा और सभी के लिए सतत विकास होगा।
माया जोशी - सीएनएस
(भारत संचार निगम लिमिटेड - बीएसएनएल - से सेवानिवृत्त माया जोशी अब सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) के लिए स्वास्थ्य और विकास सम्बंधित मुद्दों पर निरंतर लिख रही हैं)