समय ले रहा है करवट - संतोषी देवी की कविताएं
शब्द | हस्तक्षेप | साहित्यिक कलरव
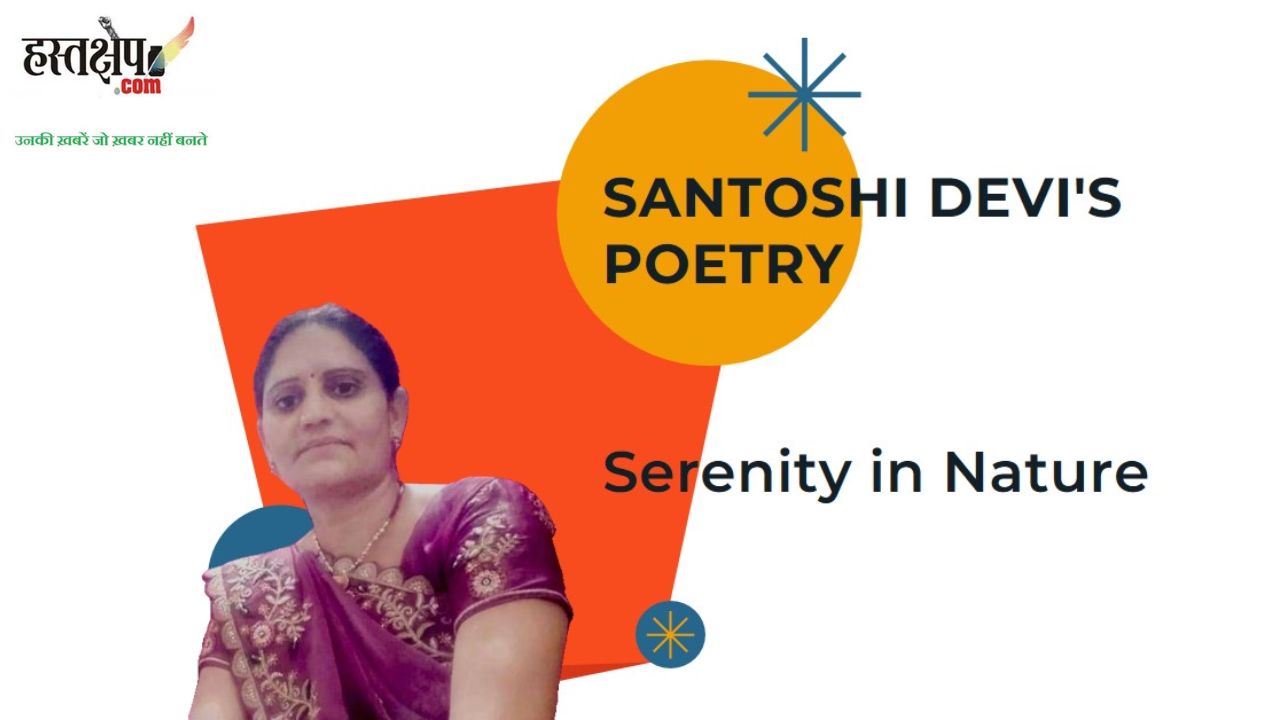
xr:d:DAFneAWvhc0:9,j:7375040158971398011,t:23070711
(1)
समय ले रहा है करवट
—————-
उनकी नजर में
वे औरतें हैं
जिन पर काबिज हैं पुरुष
शासक के माफिक।
आजमा रहे हैं आज खुद भी
वही हंटर
जिसने इनकी पीठ पर
छोड़ रखी हैं
गुलामी की
अमिट निशानियां।
फिर से पिलाने लगे हैं तेल
जो सदियों से
पीता आया है लहू
रक्त रंजित रहा है हाथ
बरसाता रहा
सत्ता के मद में
मजलूमों की पीठ पर।
और बूंद बूंद रक्त से भरता रहा
महत्वाकांक्षाओं के कटोरे।
गुलामों की जमात से
हुए थे पुरुष आजाद
स्त्रियों की बिरादरी होती तो
ये भी हो जातीं आजाद।
फिर भी सहलाती हैं
कोमल हथेलियों से पीठ
करती हैं प्रेम
हवाओं में घोलती हैं नमी
बर्फ को पिघला कर
बनती रही है झील
और कोख में पालती हैं
एक फौलादी सीना
जिस पर पड़ते ही
छूट जाता है हाथ से हंटर
तानाशाह हो जाता है
निहत्था।
और
स्त्रियां खिलखिला पड़ती हैं।
समय ले रहा करवट।
(2)
आखेटक
————-
हर बार की तरह
इस बार भी
लौटना पड़ा तुम्हें
फिर से उल्टे पाँव।
बंद हो जाता हृदय से स्पंदन
और समर्पण का महत्व
अगर पा जाती आज
भरी हुई लालसाएं
भूले से भी सुकून की ठाँव।
तुम देखते थे मुझमें
अपनी इच्छाओं की
सम्पूर्ण हरीतिमा
नीलिमा
लालिमा।
पा सकते थे शायद
लेकिन आये थे
इस बार भी
हर बार की तरह,
तुम
आखेटक बनकर।
(3)
मिटा दो अपने लिखे को।
——————-
कौन जान पाया है
हमारा समर्पण
और सपने
कसमसाता मन
निढ़ाल तन
जिस पर
हावी होती आई है
दूषित
मानसिकता।
सदियाँ गुजर गई
पीड़ाएँ भोगती रहीं
वहाँ जहाँ
लिख दिए तुमने ही
नारी के लिए छली जज्बात
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते
रमन्ते तत्र देवता
नारी ने
न्यौछावर कर दिया
माँ
बहन
बेटी
हर रूप में
बड़ी शिद्दत और
विश्वास के साथ।
फिर भी
वह रही
उपेक्षित
पीड़ित
अपने ही घर
अपनों में ही।
अब अच्छा है
मिटा दो अपने लिखे को
क्योंकि अब अति को
भोग चुकी है नारी।
(4)
चुप्पी।
————-
बोलते रहने पर
सीख जाएं विद्रोह
और बन जाएं समझदार
उससे पहले ही
करा दिया जाता है चुप।
इसीलिए
स्त्रियों का बोलना
और न बोलना
सीमित है
पुरुष सत्ता की
खींची गईं लक्ष्मण रेखा तक।
शायद पता होना चाहिए कि
नदी का कलकल
एक उसी का होना नहीं
आसपास पनपते जीवन की
सच्चाई है
जो करती है जमी को उर्वरा।
एक स्त्री की चुप्पी के साथ
चुप हो जाते हैं
घर के सभी
खिड़की
दरवाजे
दीवार,
छत
हंसी- खुशी
मुस्कान और
सब रिश्ते-नाते
तीज त्यौहार।
(5)
फांचरा।
———-
बराबर ढो तो रही है वजन
गाड़ी का एक पहिया बनी
वह औरत
फिर भी
ठोंका जाता है फांचरा
बार-बार उसी की तरफ का
दकियाई जाती है
हर बार
बिना किसी कसूर पर।
और कहते हुए
गर्माता है पुरुषत्व
रांड का चांचरा
और गाड़ी का फांचरा
समय-समय पर ठुकते
रहने चाहिये।
लेकिन हंसी आती है मुझें
उसकी खोई
याददाश्त पर
गाड़ी के फांचरे में
एक पहिया ही नहीं
दूसरा भी आता है।
(6)
भगवा
—————
जब
बरसता है बादल
नहाता है पूरा आसमान
इंद्रधनुषी रंगों में
और खींच लेता है
धरती का ध्यान अपनी ओर
झूम उठता है पूरा जीव जगत।
हर्षविभोर
नाचता है मोर
चलती हैं सुगन्धित हवाएं
इठलाते हैं
रंग बिरंगे फूल
देख खिल उठता है
रोम-रोम
खिल जाती हैं बांछें
लुटाने को प्रेम
लेकिन सहसा रुक जाती हैं
पीछे लेते हुए कदमों को
और हाथ से झरनें लगते हैं
फिसलती रेत के माफिक रंग
भिंच रही होती मुठ्ठियों के साथ
हवा हो रहे थे सप्त रंग
आसमान धुल रहा था
देखकर
तुम्हारी देह से लिपटे
केवल भगवा को।
(7)
धर्म
—
जहर ही तो था
घोल दिया मैंने
आदमी के विचार में
और धीरे धीरे घुलता
पहुँच गया सीधा
दिल दिमाग में
फैलता रहा भयंकर संक्रमण
मेरे द्वारा
एक दूसरे को
लेने लगा चपेट में
पूरे विश्व को।
सदियां बीत गईं
जड़ें और गहरी होती गईं
और आज भी सबूत है
सांप्रदायिकता
के बीच
रोती बिलखती मानवता में
इस
धर्म की
लाइलाज बीमारी के।
संतोषी देवी
शाहपुरा जयपुर राजस्थान।


