प्रतापराव कदम की कवितायें-बाजारवाद के बनाये दुःखतंत्र का सच
प्रतापराव कदम की कवितायें-बाजारवाद के बनाये दुःखतंत्र का सच
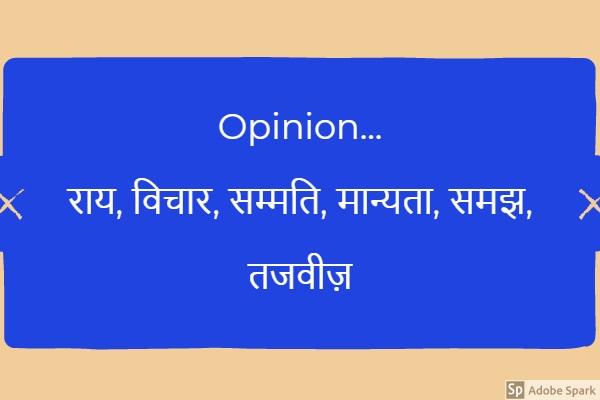
बाजारवाद के बनाये दुःखतंत्र का सच
प्रतापराव कदम की कवितायें Poems of Prataprao Kadam in Hindi.
प्रतापराव कदम की कवितायें अपने समय की आहट को भांप लेती हैं. गहराई से तंत्र के षड्यंत्र की पहचान करती हैं. दुनिया के बाहरी और भीतरी हिस्से में चल रही हलचल की सूक्ष्म पड़ताल करती हैं. हम जिस भी समय में जियें घटनाएँ हमारी जिन्दगी का हिस्सा बनकर साथ साथ चलती हैं. ऐसी ही तमाम घटनाएँ इस संग्रह की कविताओं में मौजूद हैं, जिन्हें हमने अपने समय में देखा. ऐसे तमाम हादसे हैं जिन्हें हमने अखबारों में हर रोज़ पढ़ा. कुछेक हादसों पर सोचा. कुछ पर प्रतिक्रिया की, जुलूस-जलसे, प्रदर्शन, शान्ति मार्च किए.
कदम जिस तरह हादसों का जिक्र करते हैं और जो चित्र खींचते हैं, कविताओं से गुजरते हुए वे सारे हालात हमारे मन में आशंका और कई तरह के सवाल छोड़ जाते है. कुछ संदेह, कुछ निशान, कुछ आहटें और सोचने के लिए एक नया नजरिया बेखटके दस्तक देता है कि जो हुआ वो घटनाएँ मात्र नहीं हैं. हम बीती हुई घटनाओं पर नये सिरे से सोचें, कि जो घटा है वह बिलकुल वैसा ही नहीं है जैसा हमें दिखाया या बताया जा रहा है बल्कि बहुत कुछ अनदेखा भी भीतर कहीं तलहट में दबा हुआ है,
‘निठारी तो हंडिया का एक चावल है’ ऐसी ही एक कविता है जो इंसानियत पर सवाल उठाती है और ख्यालों में किरचन छोड़ जाती है.
“चीरहरण में हाथ हमारे ही थे/ हम ही होटल ढाबे में चीखे उस पर/ मुजरे में हमने ही लुटाये रूपए/ चकलाघर तक पहुंचाने वाले हम ही थे/ हम हैं उसकी हड्डी, मज्जा, रक्त के सौदागर/ औरतों बच्चों! निठारी तो हंडिया का एक चावल है/ बच्चों औरतो! मुआफ मत करना हमें.
इसी क्रम में राजनीति को बेपर्दा करती बिलकुल सधी हुई कविताएं सिलसिलेवार मिलती है ‘उसकी कुंआर की दोपहर’ साफ़ तौर पर सत्ता प्रतिष्ठानों को दागी ठहराती है.
‘राबर्ट गिल और पारो’ एक लम्बी कविता है जिसमें अपने इतिहास और उसकी जड़ों के साथ इंसानियत को बचाए रखने की जद्दोज़हद है.
‘भरे हैं किस्से/ आहो-हरम कराहों के/ नवाब राजा-महाराजा सनक के/ युद्ध लूटपाट, मसखरी के/ चारण भात चाटुकारों के/ तिनका भर सत्य भी/ नहीं जा पाता था/ बगैर इनकी ड्योढ़ी पर धोक दिए.’
यह कविता सदियों का बोया दुःख जीती है. समय सदी को पार करके अतीत में हुई गलतियों को त्रासदी में बदल देता है. विखंडन का यह चीरता आघात एक साम्राज्यवादी साजिश के तहत हुआ. कविता नई सदी में पहुँच चुकी है. जहाँ
‘आज उलझे हैं हम ग्लोबल श्मशान में/ उस बखत भी खपती खपत में/....ऐसे में भी बची रही कहीं दूब/ हरापन नहीं/ उसे भी बाज़ार समय में लगी फफूंद.
वैश्वीकरण किस तरह हमारी खुशी और समृद्धि चर गया. कैसे हमने वैश्विक पूंजी के लिए दरवाजे खोले. इस बाज़ार ने कैसा स्वप्न दिखाया, कैसे कतरा कतरा सारी ख्वाहिशें वो लील रहा है. किस तरह रिश्तों को बर्बाद किया. जाहिर है कि नव उदारीकरण का आना कितना घातक साबित हुआ. हमने अपनी पहचान खोई. मैत्री खोई, प्रेम खोया, इंसानियत खोई. और खुदगर्जी के शिकार हुए. ‘पहले लगी वह हमारे संबंधों पर/ फिर घर पर लगी/ जगाते बाज़ार.’ किस तरह राबर्ट गिल और पारो के प्रेम का दुखद अंत हुआ. यह सब कुछ कविता सिलसिलेवार कहती जाती है. और हम सिर्फ हालात से बेबस देखते रह जाते हैं. हर घटना आँखों में ताज़ी हो उठती है. इच्छाओं को हम तिल तिल कर मरते देख कैसे सकते हैं. क्या हम निरे संवेदनहीन हो चुके हैं. ऐसे ढेरों सवाल कविता हमारे जेहन में छोड़ जाती है.
‘नीम मुल्ला खतरा-ए-ईमान’ में हमारे भीतर पैदा किये जा रहे आक्रोश पर कदम सख्त एतराज़ जताते हैं जाहिर है उन्हें मालूम है इसे सत्ता के शातिरों ने भड़काया है.
‘यह आक्रोश तुम्हारा किसके खिलाफ है/ नारे किसके ताने हुए गंडासे किसके/ किसके खिलाफ तुम्हारी यह बकवास/ दरअसल यह सब तुम्हारे अपने खिलाफ है./ और जुल्मी इनसे और ताकतवर होता है.’
हम जब तक यह समझ पायें कि असल में हुआ क्या है तब तक ताकतवर हमें छलकर हम पर ही काबिज़ हो चुके होते है. कदम इस आक्रोश को सही जगह इस्तेमाल करने के हिमायती हैं. ‘मालूम है हमें जुल्मी बहुत शातिर है/ वह तुम्हें ही इस्तेमाल कर लेता है/ तुम्हारे ही खिलाफ.’ इतना कुछ कह जाना कतई आसान नहीं है मगर फिर भी भाषा की शालीनता और कविता की मार्मिक छुअन कहीं भी ओझल नहीं होती.
‘मैं लानत भेजता हूँ मज़म्मत करता हूँ’ कहते हुए उनकी आवाज़ में एक तल्खी है. जो अपनी नासमझी में मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ उबाल है. धर्म और आस्था के अंधे लोगों के लिए नफरत साफ़ समझ में आती है. ‘थाने में देवालय’ की बात करते हुए गुनाहगारों का चेहरा आईने में ईश्वर कैसे देख रहा है इस बात को बयान करते हुए वे न्याय व्यवस्था पर गहरा तंज कसते है. ‘कांच की सडक’ तक आते आते यह बिम्ब और भी साफ हो चुका है ‘कांच की सड़क पर चलते/ अफसर, पुलिसिये, नेता, लम्पट/ कांच में नजर आता उनका असली चेहरा.’ जब चेहरा जनता की तरफ मुड़ता है तो ‘लौटते कांच की सड़क से जब/ फिर मुखौटा होता साथ उनके/ जाते यहाँ से सतर्क होकर.’
एक घटना कहीं से शुरू होती है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते सोचे समझे षड्यंत्र को पलक झपकते उजागर कर देती है. ‘अभिशाप है यह’ कहते हुए वे खोखले तंत्र की कलई खोलते हैं-
‘एक दूसरे के खिलाफ/ कितना ज़हर उगलते हैं वे/ एक दूसरे के खिलाफ/ जितना लड़ते हैं, उगलते हैं ज़हर/ उतने ही ताकतवर होते जाते हैं वे/ जितने भांजते हैं हथियार वे/ उतने ही सत्ता के नजदीक नज़र आते हैं/ वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ/ एक दूसरे को मजबूत करते हुए.’
यकीनन यहाँ जाकर कदम अपनी मंशा जता देते हैं. कि वे जुल्मतों के पहाड़ ढोती जनता के साथ खड़े हैं सत्ता के खिलाफ एक आह्वान एक मजबूत आवाज़ बनकर - ‘नहीं नहीं वरदान नहीं यह/ अभिशाप है कतई/ इस अभिशाप से कोई और नहीं करेगा मुक्त.’
यह आवाज़ ‘वाह उस्ताद’ के बहाने परत दर परत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे व्यापार का नंगा सच खोलने से नहीं चूकती –
‘इस विश्वव्यापी मंदी में/ खूब चल रही दूकान उनकी/ धर्म बिक रहा, जाति भी/ तीसरे ने खोली क्षेत्रीयता की दूकान.’
या फिर ‘साबूदाने के बड़े’ कविता में ‘वह जामवन जिसने मात दी/ बहुराष्ट्रीय कर्ड को. इसमें स्वदेशी होने का गर्व और स्वराज की भावना बसी है. किस तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और सौदागर हमारे मांस को गलाते और बेचते हैं. हमारे अस्तित्व का संकट पैदा करते हैं जहां से बच निकलने की कहीं कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही..
‘ग्राइंडर की कसौटी पर कसने से पहले/ दानों को किया आवरण मुक्त/आवरण सहित कोई किसी को/ कैसे कर सकता है आत्मसात.’
जिस तेज़ी से जोशीली और उत्साही नई पीढ़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कारखानों की चपेट में आ रही है अपना श्रम पूंजीवादी भट्टी में झोंक रही है, यह अच्छी सूचना नहीं है. हमारे मूल्य और अधिकारों पर सीधे कब्ज़ा जमाया जा रहा है. हमें आवरण मुक्त करके अपनी जड़ों से काटा जा रहा है. यह एक खतरनाक साजिश के तहत हो रहा है और हम अब भी खामोश हैं.
वे ‘अकबर शेर’ के बहाने कुछ गांठें जो कई बंदिशों में गुंथी हैं उन्हें आहिस्ते से ढीला करते हैं ये गांठें मजहब की हैं, शास्त्रों की हैं, आयतों की हैं. जिसमें कट्टरपन और हठधर्मिता भरी पड़ी है.
‘जिसने तंगखयाल के खिलाफ/ सुनीता शेरनी, सुनील शेर के शावक का नाम/ अकबर रखा/ क्या बताने के लिए कि नाम में क्या रखा है/ तो रेहाना रहीम के यहाँ गोरीप्रसाद क्यों नहीं/ और रहमत नाम क्यों नहीं/ गणेशचंद सुशीला की संतान का.’
कदम हमेशा अपनी नजर से ज़मीन की सतह पर जीती हुई बस्तियों में झांककर देखते हैं और यह अहसास दिलाते हैं कि बस्ती में जो इल्म का गोरखधंधा चल रहा है मौलाना इस सच से अनजान हैं. कि एक ही इलाके में रहने वाले तबकों के बीच ये फासले क्यूँ हैं.
‘जिस फलों के ठेकेदार ने यह मदरसा खोला है/उसके बच्चे यहाँ क्यों नहीं, कान्वेंट में क्यों/ बिहार तक के बच्चे हैं इस मदरसे में/ जो दे नहीं पाते इस बात का जवाब कि/ इस्लाम में दाढ़ी है या दाढ़ी में इस्लाम.’
इस तरह बेतकल्लुफी से सच कहना किसी चुनौती से कम नहीं है. इस कट्टर सोच से मुठभेड़ करने का साहस कदम ने किया. यह कहने की कला और जज्बा कविता में समाना बेहद कठिन है. यह कुछेक कवियों में ही देखने को मिलता है.
‘या हुसैन हाय हुसैन’ में कला की बात करते हुए हुसैन की याद में मातम मनाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय अपने जिस्म पर जो कहर बरपाता है अपनी भावना और विवेक को तकलीफ देता है लहू छलकाता है उसके खिलाफ एक मजबूत तर्क है ‘कला की आग’. कदम ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के मजहबी ढकोसले, रुढियों, खोखली आस्था पर कसकर चोट की है. उन्होंने मजहब के मुखौटे से नकली पालिश उतारकर नंगे और बदरंग सच को उघाड़ दिया.
कदम की कविताओं के और भी कई पहलू हैं, कई दरीचे हैं जिनसे वे अपनी नजर खुले आसमान की ओर ले जाते है और यह महसूस होता है कि हाशिये का दुःख तंत्र फैला पडा है. हर ओर अवसाद पसरा हुआ है. खुले आसमान के नीचे इस दम तोड़ती धरती पर. डांगरिया, दुम, विष्णु गनपत चौधुले, अब भूत पीछे उसके, ऐसी ही किस्सागोई सरीखी कवितायें है. कदम की खासियत ये है कि वो जिस परिवेश में रहते हैं जिस इलाके में सांस लेते हैं उस जगह की बात करना नहीं भूलते उनकी कविताओं में खंडवा का जिक्र कई बार आया और उसके अपने सरोकार हैं.
रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के फसादों में उलझा आम आदमी कदम की चिंता में शामिल हैं ‘किशोर त्रिपाठी की आत्महत्या’ में हम इस फ़िक्र से रूबरू होते हैं ‘मरने की अनेक जायज वजहें हैं/ ...पर बेवजह मरा किशोर त्रिपाठी/ इतना कहकर वे आगे बढ़ जाते हैं वहां ठहरते नहीं. कोई बहस की गुंजाइश नहीं, कोई हिचक नहीं. एक उम्मीद से आगे जाकर उस हद उस सिरे को पकड़ते हैं जहाँ हाशिये का तबका है जिसकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई वो हारा नहीं है. उसके पास लड़ने को हौसला है.
‘इस देश में लाखों ऐसे हैं/ जो पत्थर में इंसान बो रहे हैं/ इस बात की परवाह किये बगैर कि/ पत्थरों में स्वार्थ धड़क रहा है/ चमक रहा है स्वार्थ/ उनकी नींद में बरस रहे हैं पत्थर/ पर जी रहे हैं वे/ रोज़ निर्वासित हो रहे हैं हज़ारों/ लड़ रहे हैं वो निर्वासन के बावजूद.’
यह बताते हुए कि संघर्ष के बिना मुहाल नहीं होगा जीना भी. इस तरह वे जरूरतमंद लोगों को हक़ की लड़ाई का एक हथियार थमा देते हैं.
‘अब्दुल्ला सर का इहलोक परलोक’ की कथा सुनते हुए हम कई तरह के बदलाओं को महसूस करते हैं. एक ही किरदार इहलोक में रहते हुए भी केमिस्ट्री में परलोक की बात करता है तो यह अपने आप में किसी जुमले से कम नही है मगर कविता के भीतर चली कहानी कई मोड़ लेती है और एक पारिवारिक कथा बेहद रोचक अंदाज़ में हमारे ज़हन में एक ख़ास कोना ढूँढ़ लेती है. यही इहलोक परलोक ‘फज़र की नमाज़ के वक़्त इमलीपुरा’ में देखने को मिलता है. इस संग्रह की कवितायें आधुनिक समय के उस हिस्से को जोर से पकड़े रहती हैं जिसमें आम आदमी का दम घुट रहा है. उसे झकझोरती हैं कि अगर दिक्कतों, परेशानियों, और साजिशों को खत्म नहीं किया जा सकता, अलबत्ता नोच तो सकते ही हैं. लहुलुहान तो किया ही जा सकता है. कदम कुशल कारीगर की तरह उस व्यवस्था के बनने की तरकीब और बुनियाद को हिलाने की कोशिश करते हैं. आग का दरिया है यह कारपोरेट काल की पूंजी – जो आदमी की मेहनत और उसका खून पी रही है. वे बाजारवादी कल्चर के खिलाफ कहीं ज्यादा मुखर हैं ‘हितैषी कहाँ सब्र करते हैं’ में वे इस संस्कृति की एक प्रवृत्ति की पहले पहल पहचान करते हैं।
‘एक आदमी एक जगह से हटता है/ हवा तुरन्त खाली जगह भर देती है/....एक की आत्महत्या/ दूसरे की अनुकम्पा/ क्रियाकर्म से पहले ही हितैषी करते चर्चा/ जीते जी का संसार यह/ नहीं तो हितैषी कहाँ सब्र करते हैं.’
इस हवा को अब वे एक निश्चित आकार में तब्दील होते हुए उसे एक बाज़ार की शक्ल में ढलते देखते हैं
‘बाज़ार सत्य है कविता की तरह/ मैंने जोड़ा उसमें/ मृत्यु सत्य है विचार नहीं/ दोनों सत्य को जोड़ो तो/ बाज़ार ही सत्य है मृत्यु की तरह.’
यह आकार अब अपने भरे पूरे रंग में आता है और जिन्दगी के खात्मे यानी मृत्यु के कारणों की तफ्तीश में आगे बढ़ता है –
बाज़ार परम सत्य है/ बाज़ार परम सत्य है/ दोहराए जा रहे/ अपने को कान्धा देते हुए/ देख रहे/ अपने ही भविष्य को/ हांडी उठाये/ आगे आगे मांग के ढपडे/ दे रहे हैं/ मातम की सूचना.
इसका अगला सिरा है ‘परचून की दूकान खोलूं या स्कूल’ अब वे इस आधुनिकता के साथ संदेह से भरे हैं और तर्क करते हैं. जहां एक तरफ खामियां, तारीफ़, चाँद, समाचार, की बात करते हुए कंपनी की झूठ-बयानी का किस्सा कहते हैं वहीं दूसरी तरफ दिल दहला देने वाली हकीकत से हम वाबस्ता होते हैं –
‘एक कम्पनी अपने बीज को श्रेष्ठ बताती/ भारी मात्रा में उसकी पैदावार सफ़ेद झक कपास/ किसान लुटते पिटते मचाते शोर/ मुंहजोर कम्पनी बीज को नहीं/ कोख को देती दोष/ दर्द से इस तरह भी कांपती धरती कभी.’
अच्छी कविता वह है जो अपनी कहन कला और खूबसूरती बनाये रखे. कवित्त तभी है जब वो अपनी बात बड़ी सहजता से कह दे. कविता अपना एक पक्ष तय करती है और डटकर खड़ी रहती है कवि का कड़ा इम्तेहान यहीं होता है. कदम अपने मकसद को कभी पल भर के लिए भी नहीं भूलते. उन्हें वसंत का ज़िक्र करते हुए भी मालूम है कि क्या कहना है और किस तरह कहें कि जिसे खारिज न किया जा सके.
‘इस तरह वसंत’ में नचैया ने नाचकर/ गवैया ने गाकर/ लिख्खाड ने लिखा/ वाचक ने पढ़ दिया/ जस का तस वसंत/...
कदम एक भूमिका बुनते हैं और फिर उसे अंजाम तक ले जाते हैं –‘अध्यक्ष के काम आया/ एक रटा हुआ भाषण/ जानबूझकर बेचारे ने/ ज़िक्र नहीं किया/ ठण्ड से मरने वालों का/ छात्रों की आत्महत्या का. मगर यह छलावा क्षण भर भी टिककर नहीं रहता. एक पल में टूटकर बिखर जाता है. ‘आखिर रटा भाषण/ नई ईंट जोड़ते ही/ ढह जाता है ऐन बखत.’ कविता कहने में जैसे पारंगत और अपनी बात मनवा लेने में माहिर है. हम जब तक इसमें उलझें कि क्या कहा जाना छूट रहा है और कैसे? तब तक कदम उस पक्ष को हमारे पास लाकर एक ठसक और तल्खी से पटक देते हैं. वे कुछ इस तरह लौटते हैं जैसे किसान अभी अभी फसल काटकर अपने सर पर उठाये ढेरी का गठ्ठर देहरी में लाकर पटकता है एक खुशी और मौसम भर मेहनत की जुझारू स्मृतियों में खुद को तौलता.
‘दांत दर्द’ के बहाने से कदम अपने लक्ष्य पर उसी तरह निगाहें टिकाये रखते हैं –‘मुझे नही मालूम वे लोग कौन/ जो पकड़ते ज़िन्दगी दांतों से/ यहाँ तो दर्द ने पकड़ा दांतों को/ देह पूरी वहीं केन्द्रित.’ इस दर्द का हासिल ये है कि ये दांतों में ही सिमटकर नहीं रहता. दुनिया जहान में फैलता जाता है. एक अनूठे अंदाज़ में जिस दर्द की शुरुआत हुई वो अंत में जाकर मनुष्यता को अपने घेरे में बाँध ही लेता है. बेहद दिलचस्प और टीस के साथ एक असर छोड़ जाती यह कविता इंसानियत को ज़िंदा रखने की फ़रियाद करती है.
कदम अपनी भाषा की विश्वसनीयता, मौलिकता की पहचान और संस्कृति व संस्कार साथ लिए चलते हैं. घटनाओं की बेहिसाब फेहरिस्त में भी वे अपने करीबी कवियों को याद करते हैं. जयशंकर पसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, तसलीमा नसरीन, निराला, शमशेर, दुष्यंत कुमार, विष्णु खरे, को याद करते हुए अपनी राय साझा करते हैं. अब कोई बिलखे याकि मुरव्वत करे. कदम इस बात की जरा भी परवाह नहीं करते.
इस विमर्श में और कई फंदे, कई कई फांसे हैं हालात पूरे हिन्दुस्तान के एक जैसे हैं एक जैसी दहशत कायम है. फर्क इतना है कि कहीं हालात बद से बदतर हैं तो कहीं बहुत खराब हैं. ‘कश्मीर से कन्या कुमारी तक भारत एक है’ कविता हिन्दुस्तान के कोने कोने में औरतों पर हो रहे जुल्म की दास्ताँ सुनाती है.
अनिल पुष्कर कवीन्द्र
प्रधान संपादक
अरगला


