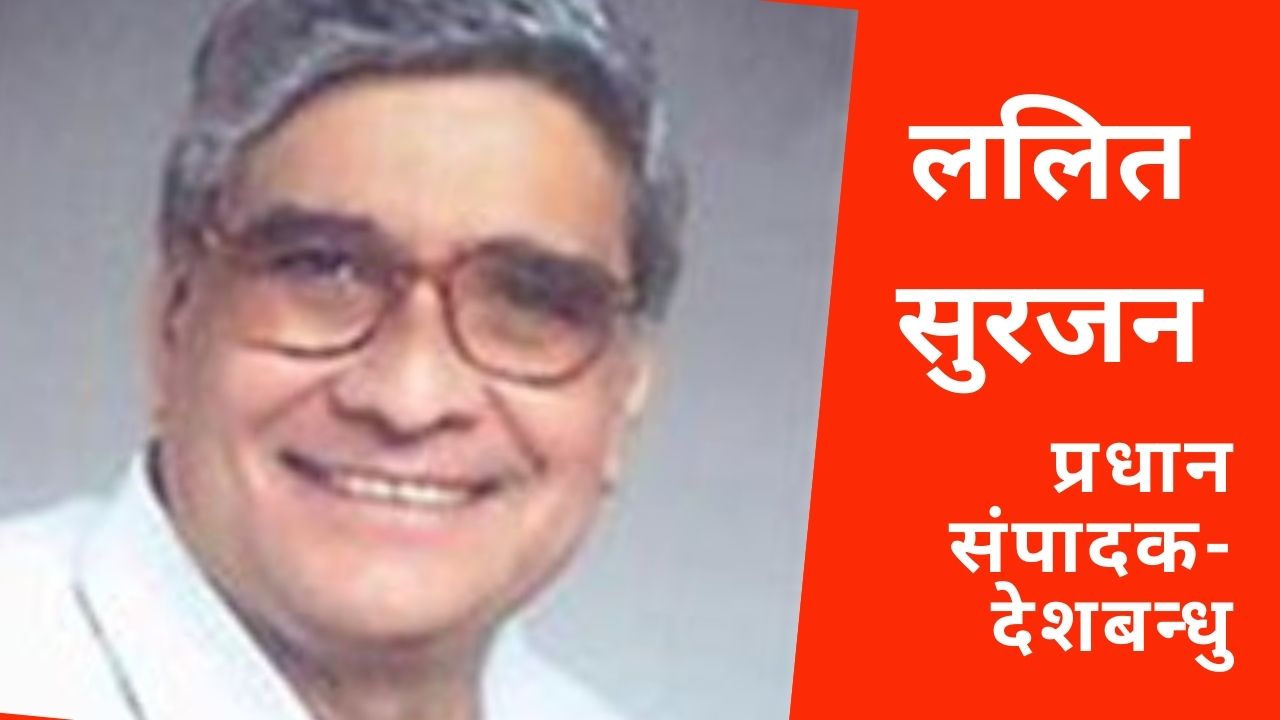लोकतंत्र का पहला खंभा बने को उतावले 5वें खंभे वाले लोग
लोकतंत्र का पहला खंभा बने को उतावले 5वें खंभे वाले लोग
ललित सुरजन
यह हर कोई जानता है कि जनतन्त्र के तीन स्तम्भ होते हैं-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों की अपनी-अपनी स्वायत्त भूमिकाएं हैं और इनके बीच इस तरह से शक्ति संतुलन होने की अपेक्षा की जाती है कि जनतन्त्र की इमारत में दरार न पड़ने पाए। इस व्यवस्था में एक नया आयाम पत्रकारिता के विकास के साथ आ जुड़ा और मीडिया को जनता के बीच चौथे स्तम्भ के रूप में मान्यता मिल गयी। ऐसी सामान्य धारणा बन गयी कि व्यवस्था के औपचारिक ढाँचे में अगर कहीं कोई कमजोरी आयेगी तो मीडिया एक सजग प्रहरी के तौर पर उसकी ओर ध्यान आकर्षित करेगा ताकि यथासमय उस कमजोरी को दूर किया जा सके। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक दौर में अखबारों ने इस रोल को पूरी गम्भीरता के साथ स्वीकार किया, आज की वास्तविकता भले ही कुछ और हो। यह याद रखना चाहिए कि औपचारिक रूप से स्थापित स्तम्भों और जनमान्यता वाले चौथे स्तम्भ के बीच कभी बहुत मधुर सम्बंध या नैकटय नहीं रहा और जब ऐसा होने लगा तो उसकी साख में कमी आने लगी।
इधर हमने देखा है कि इस संरचना में सिविल सोसायटी के नाम से एक पाँचवाँ स्तम्भ खड़ा हो गया है। इस नए स्तम्भ के निर्माण के पीछे दो मुख्य कारण दिखाई देते हैं। एक तो जनतान्त्रिक व्यवस्था की आधारभूत तासीर ही ऐसी है कि उसमें असहमति व मतवैभिन्नयता की गुंजाइश सदा बनी रहती है। दूसरे जनतन्त्र का लक्ष्य लोककल्याण होता है और उसके लक्ष्यों को पाने के लिये प्रशासन की औपचारिक सरणियाँ कभी पर्याप्त नहीं होतीं याने कार्यक्रम लागू करने के लिये एक बँधे-बँधाएं ढाँचे से बाहर निकलकर समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग लेना होता है। इस तरह सिविल सोसायटी में एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो नीतियों और मुद्दों पर प्रश्न उठाती हैं, जनतान्त्रिक सरकार को कटघरे में खडा करती हैं व उससे जवाबदेही की माँग करती हैं। दूसरी तरफ वे संस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में व्यवस्था के साथ सहयोग करती हैं। इन दोनों श्रेणियों के बीच कोई अनिवार्य विरोधाभास नहीं है बल्कि ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दोनों मोर्चों पर समान रूप से काम करती हैं।
यूँ तो सिविल सोसायटी संज्ञा का दायरा बहुत बड़ा है। उसमें छात्रसंघ, ट्रेड यूनियन, चेम्बर ऑफ कामर्स, महिला मंडल- सब आ जाते हैं, लेकिन अभी हम सिविल सोसायटी के उस बड़े और प्रमुख अंग की बात करने जा रहे हैं जिसे एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) कहा जाता है। इसका रूप इतना वृहद् हो चुका है कि अब उसे सेक्टर कहा जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर विभिन्न देशों की सरकारें इस क्षेत्र को मान्यता देती हैं व उनके साथ संवाद करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गैर सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और उनके साथ सलाह-मशविरा करते रहने से लोकहितैषी नीतियों व कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिल सकती है। कुल मिला कर एनजीओ सेक्टर को जनतन्त्र के पाँचवाँ स्तम्भ के रूप में मान्यता मिल गयी है।
भारत जैसे देश में जहाँ अभी समग्र व समावेशी विकास के लिये बहुत कुछ किया जाना बाकी है स्वाभाविक रूप से एनजीओ सेक्टर व्यापक स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। यह दिलचस्प तथ्य है कि देश के अनेकानेक राजनेताओं ने, भले ही वे किसी भी पार्टी से सम्बंध रखते हों, अपनी पहल पर ऐसे कई संगठन स्थापित कर लिये हैं। इस मामले में सरकारी अधिकारी भी पीछे नहीं हैं। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि अपने एनजीओ के माध्यम से ये लोग "इस हाथ दे उस हाथ ले" की उक्ति को चरितार्थ कर रहे हों। हम ऐसे कई फर्जी एनजीओ के बारे में जानते हैं जो सत्ताधीशों द्वारा स्थापित किये गये हैं और सरकार से किसी न किसी कार्यक्रम के नाम पर भरपूर मदद ले लेते हैं। यह एक अलग किस्सा है। अभी तो हमारी दिलचस्पी यह जानने में है कि व्यवस्था के औपचारिक ढाँचे से बाहर पाँचवें खंभे के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले एनजीओ कार्यकर्ता एकाएक पहला खंभा बनने के लिये बेताब क्यों हो उठे हैं याने वे चुनावी मैदान में क्यों कूद पड़े हैं?
एनजीओ के साथी भी इस देश के ही नागरिक हैं और उन्हें वही सारे अधिकार उपलब्ध हैं जो आपको-हमको हैं, इसलिये उनके निर्णय पर प्रश्नचिन्ह तो नहीं लगा सकते लेकिन यह जिज्ञासा मन में अवश्य उठती है कि इनकी सोच में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों आ गया है! एनजीओ सेक्टर के एक प्रमुख अभिनेता अरविंद केजरीवाल तो अब पूरी तरह से राजनेता बन ही चुके हैं, लेकिन उनके समानांतर चलने वाले या उनका अनुसरण करने वाले एनजीओ नेताओं की अब कोई कमी नहीं दिखाई देती। उदाहरण के लिये एक नाम है- जयप्रकाश नारायण का। आंध्रनिवासी श्री नारायण पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वे पिछले कई वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने लोकसत्ता नाम से एक संस्था बनाई जिसके मंच से वे चुनाव सुधारों की वकालत करते रहे हैं।
श्री नारायण ने अब लोकसत्ता को एक राजनैतिक पार्टी में तब्दील कर दिया है। वे पहले तो भाजपा के साथ गठजोड़ करने की जुगत भिड़ाते रहे। बात नहीं बनी तो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेधा पाटकर का जिक्र मैंने पिछले हफ्ते किया ही था। उनके साथ 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' में बहुत से जुझारू कार्यकर्ता भी विभिन्न स्थानों से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह एनजीओ क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे अनेक जन हैं जो राजनीति के औपचारिक मंच पर अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। इनमें से किसे कितनी सफलता मिलती है यह तो आगे चलकर पता लगेगा, लेकिन यह बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आती कि इनका राजनीति में आने का मकसद क्या है।
एक सरल उत्तर शायद यह हो सकता है कि वे जिन मूल्यों और आदर्शों के लिये अब तक संघर्षरत रहे उन्हें प्रभावी ढँग से अमल में लाने के लिये लोकसभा में बैठना जरूरी है। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने जीवन का एक लम्बा समय यूँ ही जाया किया। मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल, जयप्रकाश नारायण- ये सब नेतृत्व क्षमता के धनी लोग हैं बल्कि इनमें नेतृत्व करने की नैसर्गिक प्रतिभा है। ये अगर बीस या पच्चीस साल पहले चुनाव लड़कर लोकसभा में आए होते तो बड़े बाँधों का विरोध, सूचना का अधिकार, चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर अपने तर्क प्रभावी ढंग से सदन में रख सकते थे और उससे शायद कुछ निश्चित नतीजे भी मिलते। लेकिन हो सकता है कि यह मेरी खामख्याली हो!
मेरे मन में एक और प्रश्न उठता है कि आज देश का जो राजनैतिक वातावरण है उसमें ये कहाँ हैं? आम चुनावों के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी या जो पार्टी किसी सम्भावित गठजोड़ में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी वह अपनी घोषित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार सरकार चलाना चाहेगी। स्पष्ट है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के आर्थिक कार्यक्रम लगभग एक जैसे हैं। यह उम्मीद फिलहाल दोनों से नहीं करना चाहिए कि वे वैश्विक पूँजीवाद के एजेण्डे से हटकर काम कर पायेंगे। इन दोनों पार्टियों में अगर कोई फर्क है तो यह कि कांग्रेस बहुलतावाद में अनिवार्य रूप से विश्वास रखती है जबकि भाजपा बहुसंख्यकतावाद में। लेकिन क्या एनजीओ से जीतकर आने वालों की संख्या इतनी होगी कि वे अपने बलबूते सरकार बना सकें या गठबंधन को प्रभावित कर सकें? अगर ऐसा न हुआ तो क्या वे दो बड़ी पार्टियों के बीच कोई नया रास्ता निकालेंगे या फिर किसी एक तरफ झुक जायेंगे? उसका दीर्घकालीन परिणाम देश की राजनीति में किस रूप में सामने आयेगा?
साभार- देशबंधु